कृषि वानिकी (Agroforestry) | खेती और वृक्षारोपण का सफल संयोजन
📘 Book Title
1. कृषि वानिकी: सतत कृषि का स्मार्ट समाधान
2. Agroforestry Made Simple: किसानों के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका
3. कृषि वानिकी: खेती और वृक्षारोपण का सफल संयोजन
📙 Subtitle
• “उच्च उत्पादन, बेहतर मिट्टी, और दीर्घकालिक आय का रहस्य”
• “खेती + पेड़ = अधिक लाभ और टिकाऊ भविष्य”
• “भारतीय किसानों के लिए आधुनिक कृषि-वृक्ष मॉडल”
🌿 Tagline / Hook Line
• “एक खेत, कई आय–कृषि वानिकी से बढ़ेगी आपकी कमाई।”
• “आज लगाएं पेड़–कल पाएँ स्थायी आय।”
• “स्मार्ट किसान की पसंद—कृषि + वानिकी एक साथ।”
📝 Book Description:
कृषि वानिकी (Agroforestry) एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें खेती, पशुपालन और वृक्ष आधारित उत्पादन को एक साथ जोड़कर भूमि का अधिकतम उपयोग किया जाता है। यह पुस्तक किसानों, छात्रों, कृषि अधिकारियों और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है।
इसमें आप सीखेंगे:
-
कृषि वानिकी की मूल अवधारणा
-
पेड़ों और फसलों का सही चयन
-
वाणिज्यिक एवं पारंपरिक मॉडल
-
मिट्टी, पानी और जैव विविधता पर प्रभाव
-
भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के आसान तरीके
-
दीर्घकालिक आय और लाभ विश्लेषण
-
भारत में चल रहे सफल कृषि वानिकी मॉडल
इस पुस्तक का उद्देश्य किसानों को ऐसी प्रणाली से परिचित कराना है, जो न केवल आय बढ़ाती है, बल्कि पर्यावरण को भी लाभ पहुँचाती है। यह पुस्तक सरल भाषा, चित्रों और उदाहरणों के माध्यम से कृषि वानिकी को आसान बनाती है।
🔑 Keywords:
-
Agroforestry
-
कृषि वानिकी
-
Sustainable Farming
-
Farm Forestry India
-
Tree Based Farming
-
Silviculture
-
Multilayer Farming
-
Alley Cropping
-
Sustainable Agriculture India
-
Mixed Farming
-
Agriculture Guide Hindi
-
Indian Farming System
-
Agroforestry Models
-
Farm Income Increase
-
Climate Smart Agriculture
📘 Index / Table of Contents (सामग्री सूची)
कृषि वानिकी (Agroforestry)
भाग 1: परिचय
1.1 कृषि वानिकी का परिचय
1.2 कृषि वानिकी का महत्व
1.3 कृषि वानिकी का इतिहास और विकास
1.4 कृषि वानिकी सिस्टम का आधुनिक दृष्टिकोण
भाग 2: कृषि वानिकी के प्रकार
2.1 एग्रोसिल्वीकल्चर सिस्टम
2.2 एग्रो-पशुपालन (Agrosilvopastoral)
2.3 सिल्वोपास्टोरल सिस्टम
2.4 फार्म फॉरेस्ट्री
2.5 सोशल फॉरेस्ट्री
2.6 होम गार्डन सिस्टम
भाग 3: कृषि वानिकी के सिद्धांत और घटक
3.1 पौधों और पेड़ों का संयोजन
3.2 मिट्टी सुधार और पोषक चक्र
3.3 कृषि फसल व्यवस्थापन
3.4 जल प्रबंधन
3.5 पर्यावरणीय संतुलन
भाग 4: भूमि उपयोग और डिजाइन सिद्धांत
4.1 भूमि का चयन
4.2 साइट विश्लेषण
4.3 पेड़-फसल लेआउट
4.4 दूरी, छायांकन और रोपण पैटर्न
4.5 मॉडल डिजाइन और योजना
भाग 5: लोकप्रिय कृषि वानिकी मॉडल
5.1 भारत में अपनाए जाने वाले प्रमुख मॉडल
5.2 आल्ली क्रॉपिंग मॉडल
5.3 बाउंड्री प्लांटेशन मॉडल
5.4 ताड़-फसल मॉडल
5.5 सिल्वोपास्टोरल मॉडल
5.6 मिश्रित फसल-वृक्ष मॉडल
भाग 6: कृषि वानिकी में पौधों का चयन
6.1 फसल चयन के सिद्धांत
6.2 पेड़ प्रजातियों का चयन
6.3 नाइट्रोजन-फिक्सिंग पेड़ों का महत्व
6.4 स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुरूप चयन
6.5 व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ
भाग 7: कृषि वानिकी की स्थापना के चरण
7.1 भूमि तैयारी
7.2 रोपण सामग्री का चयन
7.3 रोपण तकनीक
7.4 सिंचाई और पोषण प्रबंधन
7.5 देखभाल और निगरानी
भाग 8: कृषि वानिकी के लाभ
8.1 पर्यावरणीय लाभ
8.2 आर्थिक लाभ
8.3 सामाजिक लाभ
8.4 जलवायु परिवर्तन में योगदान
8.5 जैव विविधता संरक्षण
भाग 9: कृषि वानिकी की चुनौतियाँ और समाधान
9.1 जल की कमी और सिंचाई समस्या
9.2 बाजार तक पहुंच
9.3 तकनीकी ज्ञान की कमी
9.4 कीट एवं रोग
9.5 समाधान और सुधार उपाय
भाग 10: कृषि वानिकी में सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ
10.1 राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, 2014
10.2 कृषि वानिकी मिशन
10.3 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम
10.4 राज्य स्तर की योजनाएँ
10.5 किसानों के लिए सब्सिडी एवं सहायता कार्यक्रम
भाग 11: कृषि वानिकी में आर्थिक लाभ और लागत विश्लेषण
11.1 लागत-लाभ विश्लेषण (Cost–Benefit Analysis)
11.2 दीर्घकालिक आय
11.3 उपज बढ़ोतरी
11.4 जोखिम और लागत प्रबंधन
11.5 बाजार और मूल्य निर्धारण
भाग 12: जोखिम प्रबंधन और संरक्षण उपाय
12.1 जलवायु जोखिम
12.2 प्राकृतिक आपदाएँ
12.3 रोग और कीटनाशक प्रबंधन
12.4 मिट्टी संरक्षण
12.5 जल संरक्षण
भाग 13: सफल केस स्टडी (Case Studies)
13.1 भारत के सफल उदाहरण
13.2 अंतर्राष्ट्रीय केस स्टडी
13.3 छोटे किसानों की सफलता
13.4 बड़े कृषि-वन मॉडल
13.5 सीखे गए प्रमुख सबक
भाग 14: भविष्य में कृषि वानिकी की संभावनाएँ
14.1 तकनीकी नवाचार
14.2 जलवायु-स्मार्ट कृषि
14.3 बायो-इकोनॉमी में योगदान
14.4 वैश्विक मांग और अवसर
14.5 नए बाजार और रोजगार अवसर
भाग 15: प्रशिक्षण और संसाधन
15.1 कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)
15.2 ICAR और ICFRE संसाधन
15.3 ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म
15.4 किसानों के लिए उपलब्ध गाइड
15.5 अनुसंधान और विकास केंद्र
भाग 16: निष्कर्ष (Conclusion)
16.1 कृषि वानिकी का भविष्य
16.2 किसान, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
16.3 स्थायी विकास की दिशा
Terminology (शब्दावली / Glossary)
A से Z महत्वपूर्ण शब्दावली
पेड़-फसल संबंधित शब्द
कृषि वानिकी तकनीकी शब्द
भूमि और पर्यावरण से जुड़े शब्द
परिशिष्ट (Appendix)
शब्दावली (Glossary)
भाग 1: परिचय — आपकी पुस्तक कृषि वानिकी (Agroforestry) के लिए पूरी तरह तैयार, सरल भाषा में और छात्रों/किसानों दोनों के लिए उपयोगी शैली में लिखा हुआ:
भाग 1: परिचय (Introduction)
1.1 कृषि वानिकी का अर्थ (Meaning of Agroforestry)
कृषि वानिकी एक ऐसी समग्र भूमि-उपयोग प्रणाली है जिसमें खेती (Agriculture), पेड़ (Forestry) और कई बार पशुपालन (Livestock) को एक साथ शामिल किया जाता है.
इसका उद्देश्य भूमि का अधिकतम उपयोग करते हुए—
-
फसल उत्पादन बढ़ाना,
-
मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना,
-
जैव विविधता बढ़ाना,
-
और किसान की आय में दीर्घकालिक वृद्धि लाना होता है.
सरल शब्दों में:
"जब खेत में फसलें और पेड़ दोनों एक साथ उगाए जाएँ, वही कृषि वानिकी है।"
1.2 कृषि वानिकी का महत्व (Importance of Agroforestry)
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि वानिकी कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है:
✔️ 1. अतिरिक्त आय का स्रोत
पेड़ किसानों को लकड़ी, फल, चारा, बांस, गोंद आदि का उत्पादन देते हैं, जिससे नियमित फसल के साथ अतिरिक्त आय मिलती है।
✔️ 2. मिट्टी का संरक्षण
पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधती हैं, जिससे कटाव (Soil Erosion) कम होता है और भूमि उपजाऊ बनी रहती है।
✔️ 3. जल संरक्षण एवं सूखा प्रबंधन
पेड़ जल को जमीन में धकेलकर भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करते हैं।
✔️ 4. जलवायु परिवर्तन में योगदान
पेड़ कार्बन को अवशोषित कर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं।
✔️ 5. पशुपालन को समर्थन
कई पेड़ चारा (fodder) प्रदान करते हैं, जिससे पशुओं का पालन कम लागत में संभव होता है।
✔️ 6. भूमि की उत्पादकता बढ़ना
मल्टी-लेयर सिस्टम से एक ही जमीन पर कई फसलों/वृक्षों का उत्पादन एक साथ होता है।
1.3 कृषि वानिकी का इतिहास (History of Agroforestry)
कृषि वानिकी कोई नई तकनीक नहीं है–यह सदियों से भारत और विश्व में प्रचलित है।
भारत में इतिहास:
-
ग्रामीण किसान पुराने समय से खेतों की मेड़ पर नीम, पीपल, बबूल, आम, करंज आदि पेड़ लगाते थे।
-
इसका उद्देश्य छाया, लकड़ी, जल संरक्षण और पालतू पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना था।
-
कुछ जनजातीय क्षेत्रों में मिश्रित खेती (Mixed Farming) और जंगल आधारित कृषि सदियों से चल रही है।
विश्व में इतिहास:
-
अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया में भूमि संरक्षण और बहुस्तरीय खेती का उपयोग पहले से किया जाता रहा है।
-
1970 के दशक में कृषि वानिकी को वैज्ञानिक रूप से एक कृषि पद्धति के रूप में पहचान मिली।
1.4 विश्व एवं भारत में कृषि वानिकी की वर्तमान स्थिति (Present Status of Agroforestry)
विश्व में:
-
अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील बड़े स्तर पर एग्रोफॉरेस्ट्री लागू कर रहे हैं।
-
FAO के अनुसार, कृषि वानिकी जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक महत्वपूर्ण समाधान है।
भारत में:
-
भारत पहला देश है जिसने 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (National Agroforestry Policy) लागू की।
-
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में पॉपलर, यूकेलिप्टस और बांस आधारित मॉडल तेजी से बढ़ रहे हैं।
-
कृषि वानिकी से किसानों की आय दुगनी करने में मदद मिली है।
भाग 2: कृषि वानिकी के सिद्धांत (Principles of Agroforestry)
भाग 2: कृषि वानिकी के सिद्धांत(Principles of Agroforestry)
कृषि वानिकी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि खेती, पेड़ और पशुपालन को किस तरह वैज्ञानिक रूप से एकीकृत किया जाए। इस भाग में हम कृषि वानिकी के सभी मौलिक सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे।
2.1 भूमि उपयोग की अवधारणा (Land-Use Concept)
भूमि (Land) किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, और कृषि वानिकी का मूल सिद्धांत भूमि का बहु-उपयोग (Multiple Use) है।
(A) एक ही जमीन का कई तरीकों से उपयोग
-
फसलें → अल्पकालिक आय
-
पेड़ → मध्यम और दीर्घकालिक आय
-
घास/चारा → पशुपालन के लिए
-
मधुमक्खी पालन → परागण और अतिरिक्त आय
इस तरह एक ही भूमि से 3–4 स्रोतों से आय मिलती है, जिसे Integrated Land-Use System कहा जाता है।
(B) भूमि का संरक्षण (Land Conservation)
कृषि वानिकी भूमि को क्षरण (soil erosion) से बचाती है।
कैसे?
-
पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधती हैं
-
पत्तियों का गिरना मिट्टी में जैविक पदार्थ (organic matter) बढ़ाता है
-
पेड़ों की छाया मिट्टी की नमी बनाए रखती है
-
हवा की गति कम होती है
इससे भूमि उपजाऊ, नम और स्वस्थ रहती है।
(C) भूमि की क्षमता (Carrying Capacity) बढ़ाना
कृषि वानिकी से:
-
एक ही समय में कई उत्पादन
-
मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है
-
भूमि का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है
2.2 फसल–पेड़ संबंध (Crop–Tree Interactions)
पेड़ और फसल दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनका संबंध 3 प्रकार से समझा जाता है:
(A) रोशनी (Light) का प्रभाव
पेड़ों की छाया यदि ज्यादा हो जाए तो फसल का विकास धीमा हो सकता है। इसलिए—
-
पेड़ों की दूरी
-
छँटाई (Pruning)
-
पेड़ की ऊँचाई
सही रखना ज़रूरी है।
उदाहरण:
-
पॉपलर (Poplar) → कम छाया → गेहूँ, सरसों, आलू के साथ अनुकूल
-
नीम, बरगद → ज्यादा छाया → फसलें कम उग पाती हैं
(B) पानी (Water Competition)
पेड़ और फसल दोनों पानी लेते हैं। यदि दूरी कम हो, तो पानी के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
समाधान:
-
पेड़ों को खेत की मेड़ पर लगाना
-
ड्रिप सिंचाई
-
गहरी जड़ वाले पेड़ चुनना
(C) पोषक तत्व (Nutrients)
पेड़ मिट्टी में पोषक तत्व जोड़ते भी हैं और उपयोग भी करते हैं।
पेड़ कैसे पोषक तत्व जोड़ते हैं?
-
पत्तियाँ गिरने पर ह्यूमस बनता है
-
नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़ (जैसे करंज, सिसम, शिरीष)
-
जैविक गतिविधि बढ़ती है
कब समस्या होती है?
-
यदि पेड़ बहुत घने हों
-
यदि एक ही पोषक तत्व की अत्यधिक मांग हो
2.3 जलवायु और मिट्टी का प्रभाव (Impact of Climate and Soil)
(A) जलवायु (Climate)
कृषि वानिकी जलवायु के अनुसार योजना बनाती है।
-
शुष्क क्षेत्र (Dry Zone): बबूल, करंज, नीम
-
आर्द्र क्षेत्र (Humid Zone): नारियल, सुपारी, काजू
-
पहाड़ी क्षेत्र: चीड़, देवदार, सेब के पेड़
(B) मिट्टी (Soil Type)
पेड़ों और फसलों की सफलता मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है।
| मिट्टी | उपयुक्त पेड़ | उपयुक्त फसलें |
|---|---|---|
| दोमट | पॉपलर, सिसम | गेहूँ, दालें |
| बलुई | यूकेलिप्टस, बबूल | बाजरा, मूंग |
| काली मिट्टी | नीम, आम | कपास, सोयाबीन |
(C) सूक्ष्म जलवायु (Microclimate)
पेड़ खेत के भीतर एक बेहतर सूक्ष्म-जलगत वातावरण बनाते हैं:
-
तापमान कम करते हैं
-
नमी बढ़ाते हैं
-
हवा की गति कम करते हैं
इससे फसलें बेहतर विकसित होती हैं।
2.4 जैव विविधता में योगदान (Contribution to Biodiversity)
कृषि वानिकी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जैसा वातावरण बनाती है।
(A) मिट्टी के जीव (Soil Microorganisms)
-
जीवाणु
-
फंगी
-
केंचुए
इनकी संख्या बढ़कर मिट्टी उपजाऊ बनती है।
(B) पक्षियों और कीटों का संरक्षण
पेड़ों से पक्षियों को घर मिलता है → वे हानिकारक कीट खाते हैं → फसल सुरक्षित
इससे कीटनाशकों की जरूरत कम होती है।
(C) परागण (Pollination) में वृद्धि
मधुमक्खियाँ और तितलियाँ पेड़ों और फूलों की ओर आकर्षित होती हैं, जिससे—
-
परागण बढ़ता है
-
फसल उत्पादन बढ़ता है
(D) प्राकृतिक शत्रु (Natural Enemies) की बढ़ोतरी
पेड़ों पर
-
मकड़ियाँ
-
लेडी बग
-
शिकारी कीट
रहते हैं, जो फसल के कीटों को नियंत्रित करते हैं।
भाग 3: कृषि वानिकी के मुख्य प्रकार(Major Types of Agroforestry Systems)
कृषि वानिकी की कई प्रणालियाँ होती हैं, जिनका चयन जलवायु, भूमि, किसान की आवश्यकता और आर्थिक लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। इस भाग में हम सभी प्रमुख प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।
3.1 एग्रो–सिल्वीकल्चर प्रणाली (Agro-Silviculture System)
यह प्रणाली फसल (crops) और पेड़ (trees) को एक साथ उगाने पर आधारित है।
यह भारत में सबसे अधिक अपनाई जाने वाली कृषि वानिकी प्रणाली है।
(A) इसकी मुख्य विशेषताएँ
-
खेतों में पेड़ों की कतारें और बीच में फसलें
-
भूमि का अधिकतम उपयोग
-
अल्पकालिक (फसल) + दीर्घकालिक (पेड़) आय
-
मिट्टी संरक्षण और नमी बढ़ाना
(B) पेड़ और फसलों का सर्वोत्तम संयोजन
| पेड़ | उपयुक्त फसलें |
|---|---|
| पॉपलर | गेहूँ, सरसों, आलू, गन्ना |
| यूकेलिप्टस | बाजरा, मूंगफली |
| नीम | चना, गेंदा |
| करंज | दालें, सब्जियाँ |
| आम | हल्की छाया वाली फसलें |
(C) लाभ
-
एक ही खेत से दो आय
-
छाया और हवा से फसल संरक्षण
-
लकड़ी, ईंधन और चारा उपलब्ध
-
खेती की लागत कम
(D) नुकसान
-
छाया यदि अधिक हो जाए तो उत्पादन कम
-
प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने के लिए छँटाई आवश्यक
3.2 एग्रो–पशुपालन प्रणाली (Agro-Pastoral System)
इस प्रणाली में फसल + घास/चारा + पशुपालन को शामिल किया जाता है।
यह प्रणाली उन किसानों के लिए है जिनके पास गाय–भैंस–बकरी जैसे पशु अधिक हैं।
(A) इसकी संरचना
-
रबी/खरीफ फसलें
-
चारा घासें
-
चारागाह भूमि
-
पशुओं का पालन
(B) उपयुक्त चारा घासें
-
नेपियर
-
बरसीम
-
गिनी घास
-
लक्खी घास
(C) लाभ
-
दूध उत्पादन बढ़ता है
-
चारा और भोजन का स्थायी स्रोत
-
मवेशियों का गोबर → जैविक खाद
-
पशुपालन से अतिरिक्त आय
3.3 सिल्वो–पेस्टोरल प्रणाली (Silvopastoral System)
यह प्रणाली पेड़ + घास + पशुपालन का मिश्रण है। इसमें फसलें शामिल नहीं होतीं।
(A) प्रमुख तत्व
-
चारागाह पेड़ (fodder trees):
→ सबबुल, शिरीष, करंज, बबूल -
घास
-
पशुधन
(B) इसके लाभ
-
पशुओं के लिए सस्ता चारा
-
जमीन का स्थायी उपयोग
-
मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि
-
पेड़ की लकड़ी अतिरिक्त आय देती है
3.4 एग्रो–हॉर्टी–सिल्वी प्रणाली (Agro-Horti-Silvi System)
यह प्रणाली तीन स्तरों पर काम करती है:
(1) फलदार पेड़ (Horti)
(2) लकड़ी/चारा देने वाले पेड़ (Silvi)
(3) फसलें या सब्जियाँ (Agro)
इसे तीन-स्तरीय कृषि वानिकी प्रणाली भी कहते हैं।
(A) संरचना का उदाहरण
-
ऊपरी स्तर: आम, अमरूद, संतरा
-
मध्य स्तर: करंज, सिसम, ग्लिरिसिडिया
-
निचला स्तर: हल्की फसलें (गेंदा, दालें, सब्जियाँ)
(B) यह किन किसानों के लिए उपयुक्त है?
-
छोटे किसान
-
बागवानी + खेती दोनों करना चाहें
-
दीर्घकालिक आय की तलाश
(C) लाभ
-
एक ही भूमि पर 3 प्रकार की उपज
-
फल से नियमित आय
-
लकड़ी से लंबी अवधि में उच्च लाभ
-
फसल से त्वरित आय
3.5 मल्टीलेयर फार्मिंग (Multi-Layer Farming)
यह प्रणाली विभिन्न ऊँचाइयों पर फसलें/पेड़ उगाने पर आधारित है।
(A) परतों (Layers) के प्रकार
| स्तर | फसलें/पेड़ |
|---|---|
| ऊपरी परत | नारियल, सुपारी, आम |
| मध्य परत | केला, अमरूद |
| झाड़ी परत | अदरक, हल्दी |
| जमीनी परत | पालक, मेथी |
| भूमिगत | आलू, अरबी |
(B) फायदे
-
जगह का 100% उपयोग
-
5–6 फसलें एक साथ
-
जोखिम कम
-
आय निरंतर मिलती है
(C) यह कहाँ लोकप्रिय है?
-
केरल
-
पश्चिम बंगाल
-
असम
-
पूर्वोत्तर भारत
3.6 एल्ली क्रॉपिंग (Alley Cropping)
इस प्रणाली में पेड़ों की कतारों (alleys) के बीच फसलें उगाई जाती हैं।
(A) उपयुक्त पेड़
-
ग्लिरिसिडिया
-
लेयुकेना
-
मोरिंगा
-
करंज
(B) एल्ली क्रॉपिंग क्यों लोकप्रिय है?
-
हवा से संरक्षण
-
मिट्टी की नमी बेहतर
-
पत्तियाँ → हरी खाद
-
जैविक खेती के लिए उपयुक्त
3.7 होम–गार्डन प्रणाली (Home Garden System)
इसे बांग्लादेश, केरल और पूर्वोत्तर में कुटीर कृषि वानिकी कहते हैं।
(A) विशेषताएँ
-
घर के आसपास फल–सब्जियाँ–औषधीय पौधे
-
नारियल, केले, पपीता
-
सब्जियाँ, मसाले
-
औषधीय पौधे
यह प्रणाली छोटे किसानों या सीमित भूमि वाले परिवारों के लिए श्रेष्ठ है।
3.8 बांस आधारित कृषि वानिकी (Bamboo-Based Agroforestry)
भारत में बांस बेहद लाभकारी फसल है।
(A) उपयोग
-
फर्नीचर
-
पेपर उद्योग
-
कंस्ट्रक्शन
-
चारा
(B) उपयुक्त संयोजन
-
बांस + अदरक
-
बांस + हल्दी
-
बांस + दालें
3.9 शुष्क क्षेत्र कृषि वानिकी (Dryland Agroforestry)
सूखे क्षेत्रों में निम्न पेड़ उपयुक्त हैं:
-
बबूल
-
करंज
-
नीम
-
खैर
फसलें: बाजरा, तिल, मूंगफली
भाग 4: फसल और वृक्ष प्रबंधन(Crop & Tree Management)
कृषि वानिकी की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है—
➡️ पेड़ों का सही चयन
➡️ फसलों का अनुकूल संयोजन
➡️ सिंचाई, पोषण, प्रूनिंग, कीट नियंत्रण का वैज्ञानिक प्रबंधन
इस भाग में हम इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे।
4.1 पेड़ प्रजातियों का चयन (Selection of Tree Species)
कृषि वानिकी में किसी भी पेड़ का चयन निम्न आधारों पर किया जाता है:
(A) जलवायु और मिट्टी के अनुसार
-
दोमट: पॉपलर, सिसम, करंज
-
बलुई: यूकेलिप्टस, बबूल
-
काली मिट्टी: आम, नीम
(B) पेड़ की बढ़वार (Growth Habit)
-
तेज़ बढ़ने वाले पेड़ → पॉपलर, यूकेलिप्टस
-
मध्यम गति वाले → करंज, सिसम
-
धीमे बढ़ने वाले → सागौन, शीशम
(C) छाया का स्तर
-
हल्की छाया वाले पेड़ → फसलें आसानी से उगती हैं
-
घनी छाया वाले पेड़ → सब्जियाँ और अनाज प्रभावित
(D) जड़ों की गहराई
-
गहरी जड़ वाले पेड़ (Tap-root) → फसलों से कम प्रतिस्पर्धा
→ नीम, सिसम -
सतही जड़ वाले पेड़ → प्रतिस्पर्धा अधिक
→ बबूल, यूकेलिप्टस
(E) किसान के लक्ष्य के अनुसार चयन
| लक्ष्य | पेड़ |
|---|---|
| लकड़ी | पॉपलर, सागौन, यूकेलिप्टस |
| फल | आम, अमरूद, किन्नू |
| चारा | करंज, ग्लिरिसिडिया, शिरीष |
| बायोफ्यूल | करंज, जेट्रोफा |
| पर्यावरण संरक्षण | नीम, बबूल |
4.2 फसलों के चयन के सिद्धांत (Selection of Crops in Agroforestry)
पेड़ और फसलों का चयन एक-दूसरे के अनुकूल होना चाहिए।
(A) छाया सहनशीलता (Shade Tolerance)
छाया सहनशील फसलें: हल्दी, अदरक, हरी सब्जियाँ
धूप पसंद करने वाली फसलें: गेहूँ, सरसों
(B) जल आवश्यकता
कम पानी वाली फसलें → बाजरा, चना
अधिक पानी वाली → गन्ना, धान
(C) आर्थिक लाभ
-
उच्च मूल्य वाली सब्जियाँ
-
मसाले
-
औषधीय पौधे
(D) मौसम की अनुकूलता
पेड़ों के बढ़ने के समय पर भी ध्यान देना चाहिए।
(E) मिट्टी की उर्वरकता
-
दलहन (Legumes) → नाइट्रोजन बढ़ाते हैं
-
अनाज → अधिक पोषक तत्व लेते हैं
4.3 पोषण प्रबंधन (Nutrient Management)
पेड़ और फसल दोनों को पोषण की जरूरत होती है।
(A) जैविक खाद (Organic Manure)
-
गोबर खाद
-
कम्पोस्ट
-
वर्मी कंपोस्ट
-
हरी खाद
पेड़ों की पत्तियाँ भी ह्यूमस बनाकर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती हैं।
(B) रासायनिक उर्वरक
इनका उपयोग फसल की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, लेकिन—
पेड़ और फसल दोनों की अलग-अलग जरूरतें होती हैं।
(C) नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़
करंज, शीशम, गुल्मोहेर
→ ये मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ते हैं।
(D) माइक्रोन्यूट्रीएंट्स
-
जिंक
-
आयरन
-
बोरॉन
पेड़ों और सब्जियों के लिए आवश्यक हैं।
4.4 कीट एवं रोग प्रबंधन (Pest & Disease Management)
कृषि वानिकी जैविक कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है।
(A) जैविक नियंत्रण (Biological Control)
पेड़ प्राकृतिक शत्रुओं को आकर्षित करते हैं:
-
लेडी बर्ड
-
मकड़ियाँ
-
शिकारी कीट
ये फसल के कीटों को खाते हैं।
(B) कीटनाशकों का जिम्मेदार उपयोग
-
न्यूनतम मात्रा
-
फसल–विशिष्ट कीटनाशक
-
पेड़ों के तने को बचाकर स्प्रे करें
(C) रोग प्रबंधन
-
पानी का जमाव न होने दें
-
समय पर छँटाई
-
संक्रमित पेड़/शाखा को हटाएँ
(D) Integrated Pest Management (IPM)
-
जैविक + रासायनिक + यांत्रिक
-
नियमित निरीक्षण
-
फेरोमोन ट्रैप
4.5 सिंचाई एवं जल संरक्षण तकनीक (Irrigation & Water Management)
पेड़ और फसलों के बीच पानी के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए उचित जल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
(A) ड्रिप सिंचाई (Drip Irrigation)
सबसे अच्छा विकल्प:
-
पानी की बचत
-
जड़ों तक सीधी नमी
-
मल्चिंग के साथ बेहतर परिणाम
(B) स्प्रिंकलर सिंचाई
विस्तृत क्षेत्रों में लागू
फसल + पेड़ → दोनों को समान पानी
(C) रेन वाटर हार्वेस्टिंग
-
खेत तालाब
-
मेड बंधान
-
चेक डैम
(D) मल्चिंग
-
सूखी पत्तियाँ
-
पौधों के अवशेष
-
घास
→ मिट्टी की नमी बढ़ती है
→ खरपतवार कम होते हैं
4.6 छँटाई (Pruning) और पेड़ प्रबंधन
प्रूनिंग कृषि वानिकी की रीढ़ है।
(A) क्यों आवश्यक है?
-
छाया को नियंत्रित करने के लिए
-
हवा का प्रवाह बढ़ाने के लिए
-
रोग और कीट कम करने के लिए
-
लकड़ी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए
(B) छँटाई के प्रकार
-
फॉर्मेटिव प्रूनिंग
→ पेड़ को सही आकार देना -
शीर्ष छँटाई (Crown Reduction)
→ पेड़ के ऊपरी भाग को संतुलित करना -
साइड ब्रांच हटाना
→ फसलों को अधिक सूर्य प्रकाश
4.7 प्रतिस्पर्धा प्रबंधन (Competition Management)
पेड़–फसल प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने के उपाय:
-
उचित दूरी
-
सही प्रूनिंग
-
उर्वरकों का सही वितरण
-
नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़
-
माइक्रो सिंचाई
4.8 फसल चक्र (Crop Rotation) और मिश्रित खेती
-
दलहनी → नाइट्रोजन बढ़ाती है
-
सब्जियाँ → मूल्यवान फसलें
-
अनाज → मुख्य खाद्य फसलें
फसल चक्र मिट्टी को स्वस्थ रखता है।
भाग 5: लोकप्रिय कृषि वानिकी मॉडल(Popular Agroforestry Models)
भारत और विश्व में कई तरह के कृषि वानिकी मॉडल अपनाए जाते हैं। प्रत्येक मॉडल का उद्देश्य भूमि का अधिकतम उपयोग, आय में विविधता और पर्यावरणीय सुधार करना है। नीचे सबसे उपयोगी और लोकप्रिय मॉडल दिए गए हैं।
5.1 कृषि-वृक्षारोपण मॉडल (Agrisilviculture Model)
इस मॉडल में किसान एक ही खेत में फसलें + वृक्ष उगाते हैं। यह भारत में सबसे लोकप्रिय मॉडल है।
मुख्य विशेषताएँ
-
फसल और वृक्ष एक दूसरे का समर्थन करते हैं
-
वृक्षों की छाया, हवा से सुरक्षा, नमी संरक्षण
-
दीर्घकालीन (पेड़) + त्वरित (फसल) आय
लोकप्रिय वृक्ष–फसल संयोजन
-
नीम + गेहूँ
-
यूकेलिप्टस + सोयाबीन
-
पॉपलर + गन्ना
-
आम + दलहन फसलें
लाभ
-
आय के दो स्रोत
-
मिट्टी की उर्वरता में सुधार
-
फसल विफलता का जोखिम कम
5.2 कृषिवानिकी-पशुपालन मॉडल (Agrosilvipastoral Model)
इस मॉडल में फसलें + वृक्ष + चारा घास + पशुपालन सभी साथ में जोड़े जाते हैं।
बेस्ट फॉर:
-
छोटे किसानों के लिए
-
बंजर/सूखे क्षेत्रों के लिए
मुख्य तत्व
-
पेड़: अरदू, सूबबूल, नेम
-
फसल: बाजरा, ज्वार
-
चारा: नेपियर घास
-
पशु: गाय, बकरी, भैंस
लाभ
-
दूध + लकड़ी + अनाज + चारा—चार आय स्रोत
-
खेत की उत्पादकता कई गुना बढ़ती है
-
मिट्टी का संरक्षण और जैव विविधता में वृद्धि
5.3 कृषिवानिकी मत्स्य मॉडल (Aqua-Agroforestry / Agrosilviaquaculture)
इसमें खेत के एक हिस्से में तालाब या पानी का क्षेत्र बनाया जाता है और उसके आसपास पेड़ व फसलें उगाई जाती हैं।
सिस्टम संयोजन
-
तालाब में: मछली पालन
-
किनारों पर: केला, नारियल, सुपारी
-
आसपास: चारा और सब्जी उत्पादन
लाभ
-
पानी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग
-
उच्च लाभदायक (fish + fruit)
-
ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय मॉडल
5.4 बाउंड्री / मेंड़ वानिकी मॉडल (Boundary Plantation Model)
इसमें खेत के चारों ओर मेंड़ों पर पेड़ लगाए जाते हैं। यह सबसे आसान मॉडल है।
लोकप्रिय वृक्ष प्रजातियाँ
-
नीलगिरी
-
बबूल
-
शीशम
-
खेजड़ी
-
करंज
लाभ
-
फसल क्षेत्र में कमी नहीं
-
खेत को हवा, मृदा कटाव से सुरक्षा
-
लकड़ी, ईंधन और चारे की उपलब्धता
5.5 होम गार्डन कृषि वानिकी (Homegarden Agroforestry)
यह दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्व और केरल में सबसे अधिक प्रचलित है। इसमें घर के आसपास कई स्तरों (layers) में पेड़, सब्जियाँ, फलदार पौधे और मसाले उगाए जाते हैं।
मुख्य संरचना
-
ऊपरी स्तर: नारियल, कटहल
-
मध्य स्तर: केला, अमरूद
-
निचला स्तर: सब्जियाँ, मसाले, औषधीय पौधे
लाभ
-
पूरे वर्ष विविध उत्पादन
-
पोषण सुरक्षा
-
कम भूमि में भी अधिक उत्पादन
5.6 पॉपलर/यूकेलिप्टस-आधारित मॉडल (Poplar & Eucalyptus Based Agroforestry)
उत्तर भारत में यह मॉडल तेजी से बढ़ा है क्योंकि ये तेजी से बढ़ने वाले पेड़ हैं।
फसल संयोजन
-
गेहूँ
-
गन्ना
-
सरसों
-
चारा
लाभ
-
5–6 वर्षों में लकड़ी से बड़ा लाभ
-
उद्योगों में उच्च मांग
-
कम रखरखाव लागत
5.7 फलदार पेड़ आधारित मॉडल (Horticulture-based Agroforestry)
इसमें फलों के बगीचों के बीच फसलें उगाई जाती हैं।
लोकप्रिय फलदार पेड़
-
आम
-
अमरूद
-
नींबू
-
पपीता
में इंटरक्रॉपिंग
-
दालें
-
सब्जियाँ
-
हल्दी
-
अदरक
लाभ
-
छोटी और लंबी अवधि की आय
-
मिट्टी की सेहत में सुधार
5.8 शुष्क क्षेत्रों के लिए सिल्वोपाश्चर मॉडल (Silvopastoral Model)
सूखे क्षेत्रों में घास + पेड़ का संयोजन सबसे बेहतर है।
उपयोगी पेड़
-
खेजड़ी
-
बबूल
-
रोहिड़ा
घास
-
स्टायलो
-
सीटन घास
लाभ
-
चराई के लिए उत्कृष्ट
-
पशुपालन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत
5.9 बहुस्तरीय मॉडल (Multistoried Model / Layered Agroforestry)
इसमें एक ही स्थान पर 3–4 स्तरों पर पौधे लगाए जाते हैं।
उदाहरण
-
नारियल → केला → सब्जियाँ → औषधीय पौधे
लाभ
-
कम भूमि में अधिक उत्पादन
-
अधिक प्रकाश और नमी का उपयोग
5.10 शहरी कृषि वानिकी मॉडल (Urban Agroforestry)
शहरों में छतों, छोटे बगीचों और खाली स्थानों में पेड़, सब्जियाँ और औषधीय पौधे उगाने का बढ़ता चलन।
लाभ
-
प्रदूषण में कमी
-
स्वस्थ आहार स्रोत
-
आत्मनिर्भरता
भाग 6: कृषि वानिकी में पौधों का चयन
भाग 6: कृषि वानिकी में पौधों का चयन(Plant Selection in Agroforestry)
कृषि वानिकी में सफल परिणाम काफी हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन से पेड़, फसलें, घास और झाड़ियाँ खेत की जलवायु, मिट्टी और किसान की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार चुनी जाएँ।
सही पौधों का चयन खेती को लाभदायक, टिकाऊ और दीर्घकालिक बनाता है।
6.1 पौधों के चयन के मुख्य सिद्धांत (Key Principles of Plant Selection)
(1) स्थानीय जलवायु के अनुसार चयन
-
वर्षा की मात्रा
-
तापमान
-
आर्द्रता
-
हवा की तीव्रता
उदाहरण:
-
शुष्क क्षेत्रों में → खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल
-
आर्द्र क्षेत्रों में → नारियल, सुपारी, काली मिर्च
(2) मिट्टी के प्रकार के अनुसार चयन
-
दोमट → अधिकांश फलदार वृक्ष
-
रेतीली मिट्टी → खेजड़ी, अरदू
-
काली मिट्टी → नीम, आम, बांस
-
जलभराव वाली मिट्टी → जामुन, अरहर, केला
(3) फसलों पर प्रभाव (Canopy & Root Interaction)
-
पेड़ की छाया फसल पर नकारात्मक असर न डाले
-
जड़ों का अधिक विस्तार फसल से पोषक तत्व न छीने
-
पत्तियों का झड़ाव मिट्टी को जैविक पदार्थ प्रदान करे
(4) बहुउपयोगी पौधों को प्राथमिकता
ऐसे पौधे चुनें जिनसे कई तरह के लाभ मिलें:
-
लकड़ी
-
फल
-
चारा
-
औषधीय उपयोग
-
ईंधन
(5) बाजार मांग के अनुसार पौधे
-
औद्योगिक लकड़ी (पॉपलर, यूकेलिप्टस)
-
मसाले (मेथी, काली मिर्च, इलायची)
-
फलों की बाजार मांग (नींबू, अमरूद, सेब)
6.2 कृषि वानिकी में प्रयुक्त प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ (Major Tree Species Used in Agroforestry)
नीचे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सबसे लोकप्रिय और लाभदायक वृक्ष प्रजातियाँ दी गई हैं:
(A) तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष (Fast Growing Trees)
कम समय में आर्थिक लाभ देने वाले पेड़
| वृक्ष | उपयोग | अवधि |
|---|---|---|
| पॉपलर | प्लाइवुड, माचिस फैक्टरी | 5–7 वर्ष |
| यूकेलिप्टस | कागज, लकड़ी | 4–6 वर्ष |
| सूबबूल | चारा, लकड़ी | 3–4 वर्ष |
| बांस | निर्माण, फर्नीचर | 4–6 वर्ष |
(B) फलदार वृक्ष (Fruit Trees)
फसल + फल से दोहरी आय
-
आम
-
अमरूद
-
नींबू
-
केला
-
पपीता
-
अनार
-
नारियल
-
कटहल
(C) नाइट्रोजन फिक्सिंग वृक्ष (Nitrogen Fixing Trees)
मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं
-
खेजड़ी
-
बबूल
-
ग्लिरिसिडिया
-
लेयुकेना (Subabul)
-
रोहिड़ा
(D) छायादार वृक्ष (Shade Trees)
अश्वगंधा, हल्दी, अदरक जैसी फसलों के लिए श्रेष्ठ
-
शीशम
-
नीम
-
बरगद (सीलिंग plantations)
-
अर्जुन
(E) औषधीय एवं बहुउपयोगी वृक्ष
-
अर्जुन
-
नीम
-
मोरिंगा (सहजन)
-
जामुन
-
गिलोय (लता)
6.3 कृषि वानिकी में फसलों का चयन (Field Crops in Agroforestry)
(A) खाद्यान्न फसलें
-
गेहूँ
-
धान
-
बाजरा
-
मक्का
-
ज्वार
(B) दलहन फसलें — सर्वश्रेष्ठ इंटरक्रॉप
-
मूंग
-
उड़द
-
अरहर
-
लोबिया
नाइट्रोजन फिक्सेशन से मिट्टी उपजाऊ होती है।
(C) तिलहन फसलें
-
सरसों
-
सोयाबीन
-
तिल
(D) नकदी फसलें (Cash Crops)
-
गन्ना
-
कपास
-
सब्जियाँ (टोमैटो, गोभी, पालक)
6.4 घास और चारा प्रजातियाँ (Grass & Fodder Species)
कृषि वानिकी + पशुपालन मॉडल के लिए आवश्यक।
-
नेपियर घास
-
बरसीम
-
सेटन घास
-
स्टायलो
-
मुलाट्टो II
लाभ:
-
पशु पोषण सुधार
-
दोहरी आय
-
मिट्टी कटाव रोकता है
6.5 झाड़ियों और औषधीय पौधों का चयन (Shrubs & Medicinal Plants)
छोटे क्षेत्रों के लिए उत्कृष्ट संयोजन।
झाड़ियाँ
-
करौंदा
-
लेमनग्रास
-
गुड़हल
-
तुलसी
औषधीय पौधे
-
अश्वगंधा
-
एलोवेरा
-
सतावर
-
गिलोय
-
मिंट (पुदीना)
6.6 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के अनुसार पौधों का चयन (Region-wise Plant Selection)
(A) शुष्क/अर्ध-शुष्क क्षेत्र
-
खेजड़ी
-
रोहिड़ा
-
बबूल
-
बाजरा
-
मूंग
(B) आर्द्र/उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
-
नारियल
-
सुपारी
-
केला
-
काली मिर्च
-
अदरक
(C) पहाड़ी क्षेत्र
-
सेब
-
अखरोट
-
चेस्टनट
-
आलू
-
राजमा
6.7 पौधों के चयन में सामान्य गलतियाँ (Common Mistakes to Avoid)
-
बहुत अधिक छाया देने वाले पेड़ चुन लेना
-
पेड़ों के बीच पर्याप्त दूरी न रखना
-
स्थानीय जलवायु/मिट्टी को अनदेखा करना
-
केवल एक ही किस्म पर निर्भर रहना
-
बाजार की मांग का अध्ययन न करना
6.8 आदर्श पौधा संयोजन (Best Recommended Combinations)
A. पॉपलर + गेहूँ + सरसों
उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय मॉडल
B. आम का बगीचा + दालें (अरहर/मूंग)
शुरुआती 3–4 वर्षों में अच्छी आय
C. नारियल + केला + सब्जियाँ
मल्टी-स्टोरी सिस्टम
D. खेजड़ी + बाजरा + मूंग
शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम
भाग 7: कृषि वानिकी की स्थापना के चरण
(Steps to Establish an Agroforestry System)
कृषि वानिकी प्रणाली स्थापित करना एक वैज्ञानिक और चरणबद्ध प्रक्रिया है। सही योजना, सही पौधों का चयन और उचित प्रबंधन सफल और लाभदायक कृषि वानिकी की नींव हैं।
नीचे एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका दी गई है, जिसे किसान सरलता से अपनाकर अपनी जमीन पर एक मजबूत कृषि वानिकी मॉडल विकसित कर सकते हैं।
7.1 प्रारंभिक साइट मूल्यांकन (Initial Site Assessment)
सफल कृषि वानिकी की शुरुआत खेत की प्रकृति को समझने से होती है।
मुख्य बिंदु:
-
मिट्टी का प्रकार: दोमट, काली, रेतीली
-
मिट्टी की उर्वरता और pH
-
उपलब्ध जल संसाधन
-
भूमि की ढाल (slope)
-
मौसम और वर्षा पैटर्न
-
हवा की दिशा और वेग
सुझाव:
-
मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएँ
-
सूखे क्षेत्रों में जल संरक्षण संरचना की योजना बनाएं
7.2 लक्ष्य और मॉडल का चयन (Deciding the Goal & Selecting the Model)
कृषि वानिकी प्रणाली को स्थापित करने से पहले यह तय करना ज़रूरी है कि किसान का अंतिम लक्ष्य क्या है।
संभावित लक्ष्य:
-
लकड़ी उत्पादन
-
फल उत्पादन
-
चारा उत्पादन
-
सब्जियाँ
-
मछली + कृषि मॉडल
-
दीर्घकालीन + त्वरित आय वाला संयोजन
इसके अनुसार सही मॉडल चुनें:
-
एग्रीसिल्वी (फसल + पेड़)
-
एग्रोसिल्विपाश्चर (पेड़ + फसल + घास + पशु)
-
फल आधारित मॉडल
-
मल्टी-स्टोरी मॉडल
-
बाउंड्री प्लांटेशन
7.3 पौधों का चयन (Selection of Plant Species)
सही पौधों का चयन कृषि वानिकी की रीढ़ है (विस्तार भाग 6 में दिए गए हैं)।
ध्यान में रखें:
-
स्थानीय जलवायु
-
बाजार मांग
-
फसल और वृक्ष का सामंजस्य
-
नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़ सुनिश्चित करें
-
तेजी से बढ़ने वाले + दीर्घकालीन दोनों का संतुलन
लोकप्रिय संयोजन:
-
पॉपलर + गेहूँ + सरसों
-
आम + दालें
-
खेजड़ी + बाजरा
-
नारियल + केला + सब्जियाँ
7.4 भूमि तैयारी (Land Preparation)
मुख्य चरण:
-
खेत की सफाई
-
जुताई और समतलीकरण
-
उचित जल निकास व्यवस्था
-
वृक्ष रोपण के लिए गड्ढे तैयार करना
-
जैविक खाद (compost) और गोबर खाद का उपयोग
फायदा:
-
पौधों की जड़ों को बेहतर वृद्धि
-
मिट्टी संरचना में सुधार
7.5 पौध रोपण की योजना (Planting Layout & Spacing)
सही दूरी और लेआउट से फसल व वृक्ष दोनों लाभ देते हैं।
पेड़ों की दूरी (औसत):
-
पॉपलर: 8 × 4 मी
-
यूकेलिप्टस: 3 × 3 मी
-
आम: 9 × 9 मी
-
बांस: 5 × 5 मी
लेआउट के प्रकार:
-
ब्लॉक प्लांटेशन
-
बाउंड्री प्लांटेशन
-
कंटूर आधारित (ढाल वाली भूमि)
-
मल्टी-स्टोरी प्लान
ध्यान रखें:
-
फसल को पर्याप्त प्रकाश मिले
-
पेड़ों की जड़ें फसल से प्रतिस्पर्धा न करें
7.6 फसल प्रबंधन (Crop Management)
पेड़ों और फसलों को साथ उगाने के लिए नियमित निगरानी जरूरी है।
मुख्य कार्य:
-
समय पर सिंचाई
-
खरपतवार नियंत्रण
-
जैविक उर्वरक का उपयोग
-
मल्चिंग
-
पौधों की छंटाई
-
रोग एवं कीट प्रबंधन
सुझाव:
रासायनिक दवाओं के बजाय जैविक नियंत्रण उपाय अपनाएँ।
7.7 वृक्ष प्रबंधन (Tree Management Practices)
पेड़ों की देखभाल के चरण:
-
प्रारंभिक 6 महीनों में नियमित सिंचाई
-
सुरक्षा जाल/बाड़ से बचाव (पशुओं से)
-
टॉपिंग और प्रूनिंग
-
पत्तियों से बना हुआ जैविक खाद खेत में मिलाएँ
-
रोग-कीट का समय पर उपचार
वृक्ष छंटाई क्यों जरूरी है?
-
फसलों को प्रकाश मिलता है
-
वृक्षों का आकार नियंत्रित रहता है
-
ज्यादा लकड़ी उत्पादन
7.8 सिंचाई और जल प्रबंधन (Irrigation & Water Management)
बेहतर तकनीकें:
-
ड्रिप सिंचाई
-
स्प्रिंकलर
-
कंटूर ट्रेंच
-
जल संचयन तालाब
लाभ:
-
पानी की बचत
-
उत्पादकता में बढ़ोतरी
-
सूखा सहनशीलता में वृद्धि
7.9 रोग एवं कीट प्रबंधन (Pest & Disease Management)
जैविक उपाय:
-
नीम आधारित कीटनाशक
-
ट्राइकोडर्मा
-
फेरोमोन ट्रैप
-
जैव-नियंत्रक कीट
रासायनिक दवाइयाँ (केवल जरूरत पड़ने पर):
-
WHO & ICAR मानकों के अनुसार
7.10 कटाई और लाभ प्राप्ति (Harvesting & Profit Realization)
फसल कटाई:
फसलें अपने निर्धारित समय पर काटकर नियमित आय देती हैं।
वृक्ष कटाई:
-
पॉपलर: 5–7 वर्ष
-
यूकेलिप्टस: 4–6 वर्ष
-
बांस: 4–6 वर्ष
-
आम: 4–5 वर्ष में फल उत्पादन
आय के स्रोत:
-
लकड़ी
-
फल
-
फसल
-
चारा
-
औषधीय पौधे
7.11 विपणन और मूल्य संवर्धन (Marketing & Value Addition)
कृषि वानिकी में अधिक लाभ के लिए बाजार की समझ आवश्यक है।
स्मार्ट मार्केटिंग उपाय:
-
स्थानीय मंडी के बजाय थोक खरीदारों से संपर्क
-
FPO/SHG के माध्यम से बिक्री
-
फल प्रसंस्करण (जैम, जूस, पाउडर)
-
लकड़ी उद्योग से अनुबंध
7.12 दीर्घकालीन रख-रखाव (Long-term Maintenance)
-
हर वर्ष पेड़ों की छंटाई
-
मिट्टी की जांच
-
बाउंड्री पर सुरक्षा व्यवस्था
-
जैविक खाद का वार्षिक उपयोग
-
कीट/रोग की नियमित निगरानी
7.13 मॉनिटरिंग एवं सुधार (Monitoring & Improvement)
सफल कृषि वानिकी में निरंतर सुधार सबसे आवश्यक है।
क्या मॉनिटर करें?
-
पेड़ की ऊँचाई और व्यास
-
फसल की उपज
-
मिट्टी की उर्वरता
-
जल उपयोग
-
आर्थिक लाभ
भाग 8: कृषि वानिकी के लाभ(Agroforestry Benefits)
कृषि वानिकी एक बहुआयामी कृषि पद्धति है जिसमें पेड़, झाड़ियाँ, फसलें और पशुपालन—इन सभी का समन्वित प्रबंधन शामिल है। यह परंपरागत कृषि की तुलना में अधिक स्थायी, लाभदायक और पर्यावरण-सुरक्षित तरीका प्रदान करती है। नीचे कृषि वानिकी के प्रमुख लाभों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है:
8.1 आर्थिक लाभ
1. बहु-आय (Multiple Income Streams)
कृषि वानिकी में किसान को एक ही खेत से अनेक उत्पाद मिलते हैं—जैसे लकड़ी, फल, चारा, गोंद, औषधीय पत्तियाँ, मसाले, सब्जियाँ आदि। इससे आय के अधिक स्रोत बनते हैं।
2. बाजार जोखिम कम
फसलों के खराब होने पर भी पेड़ों और बागवानी उत्पादों से नियमित आय मिलती रहती है, जिससे आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है।
3. उच्च मूल्य वाले उत्पाद
नीम, सागौन, यूकेलिप्टस, आम, बरगद, खैर, अर्जुन जैसे पेड़ उच्च मूल्य के होते हैं। समय के साथ इनकी लकड़ी और उत्पादों की कीमत बढ़ती है।
4. कम लागत में उत्पादन
पेड़ों की छाया, गिरी पत्तियों और जैविक पदार्थ से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, जिससे उर्वरकों और सिंचाई पर खर्च कम होता है।
8.2 पर्यावरणीय लाभ
1. जैव विविधता में वृद्धि
कृषि वानिकी खेत में विभिन्न प्रकार के पौधे, पक्षी, कीट और सूक्ष्मजीवों को आकर्षित करती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है।
2. मिट्टी संरक्षण
पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं जिससे कटाव, अपरदन और पोषक तत्वों का नुकसान कम होता है।
3. कार्बन भंडारण (Carbon Sequestration)
पेड़ वातावरण से CO₂ को अवशोषित करके कार्बन को लकड़ी और मिट्टी में संग्रहित करते हैं। यह जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक है।
4. जल संरक्षण
पेड़ों की जड़ें पानी को मिट्टी की गहराई तक पहुँचाती हैं, भूमिगत जल पुनर्भरण (recharge) बढ़ता है और खेत की नमी संरक्षित रहती है।
8.3 सामाजिक लाभ
1. ग्रामीण रोजगार
पेड़ आधारित उद्योग जैसे लकड़ी, फल प्रसंस्करण, शहद उत्पादन, औषधीय पत्तियों के संग्रहण से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ता है।
2. किसानों में कौशल विकास
कृषि वानिकी से किसान वृक्ष प्रबंधन, बागवानी, प्रसंस्करण और विपणन जैसे नए कौशल सीखते हैं।
3. पशुधन पोषण
पेड़ों से मिलने वाला पत्तेदार चारा (fodder) पशुओं के पोषण में काम आता है, जिससे दूध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य बेहतर होता है।
8.4 कृषि उत्पादन से संबंधित लाभ
1. फसल उत्पादन में वृद्धि
पेड़ों द्वारा मिट्टी में जैविक पदार्थ और पोषक तत्त्व बढ़ने से फसल की उर्वरता और उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है।
2. सूक्ष्म जलवायु (Microclimate) सुधार
पेड़ खेत में हवा की गति, तापमान और आर्द्रता को संतुलित करते हैं जिससे फसलों की वृद्धि बेहतर होती है।
3. कीट-रोग प्रबंधन
कुछ पेड़, जैसे नीम और करंज, प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखते हैं जिससे फसल सुरक्षा बढ़ती है और रासायनिक दवाओं पर निर्भरता कम होती है।
8.5 दीर्घकालिक स्थिरता
1. भूमि की गुणवत्ता का संरक्षण
पेड़ों के लंबे समय तक रहने से भूमि में भौतिक, रासायनिक और जैविक सुधार होता है।
2. जलवायु प्रतिरोधक क्षमता
कृषि वानिकी सूखा, बाढ़, हवा जैसे प्राकृतिक जोखिमों से फसलों और खेतों को बचाने में मदद करती है।
3. स्थायी कृषि (Sustainable Agriculture)
कृषि वानिकी प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करती है और भविष्य के लिए भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखती है।
भाग 8 का सारांश (Quick Summary)
✔ कृषि वानिकी कृषि आय बढ़ाती है
✔ मिट्टी, पानी और पर्यावरण की रक्षा करती है
✔ जलवायु परिवर्तन कम करने में मदद करती है
✔ किसानों को आर्थिक और सामाजिक स्थिरता प्रदान करती है
✔ भूमि को दीर्घकालिक रूप से उत्पादक बनाए रखती है
भाग 9: कृषि वानिकी की चुनौतियाँ और समाधान
(Agroforestry Challenges & Solutions)
कृषि वानिकी (Agroforestry) एक अत्यंत लाभदायक और टिकाऊ कृषि प्रणाली है, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के दौरान कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। किसानों को इन चुनौतियों की जानकारी होना और उनके समाधान अपनाना आवश्यक है। नीचे कृषि वानिकी से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ और उनके व्यावहारिक समाधान विस्तार से दिए गए हैं।
9.1 तकनीकी चुनौतियाँ
चुनौती 1: उचित मॉडल का चयन न होना
कई किसान यह तय नहीं कर पाते कि कौन सा मॉडल (Agri-silviculture, Horti-Agri, Silvo-pastoral आदि) उनके भू-भाग के लिए उपयुक्त है।
समाधान:
-
भूमि की बनावट, जल उपलब्धता और जलवायु के अनुसार मॉडल चुनें।
-
कृषि विशेषज्ञ या कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से परामर्श लें।
-
छोटे पैमाने पर पायलट प्रोजेक्ट चलाकर परिणामों के आधार पर विस्तार करें।
9.2 पौधों का चयन और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियाँ
चुनौती 2: सही पेड़–फसल संयोजन चुनने में कठिनाई
कुछ पेड़ फसलों से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
समाधान:
-
पेड़ और फसल का संयोजन वैज्ञानिक आधार पर चुनें (जैसे — नीम + गेहूँ, मोरिंगा + दालें, सागौन + चारागाह)।
-
गहरी जड़ वाले पेड़ों को उथली जड़ वाली फसलों के साथ लगाएँ।
-
पेड़ के बीच उचित अंतराल रखें।
चुनौती 3: सिंचाई प्रबंधन में कठिनाई
पेड़ों और फसलों की जल आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं।
समाधान:
-
ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग अपनाएँ।
-
पेड़ों के लिए अलग सिंचाई लाइन रखें।
-
वर्षा जल संचयन संरचना बनाएं।
9.3 आर्थिक और बाजार से जुड़ी चुनौतियाँ
चुनौती 4: शुरुआत में निवेश अधिक लगना
पौध की कीमत, सिंचाई और संरचना पर प्रारंभिक लागत अधिक होती है।
समाधान:
-
सरकार की “कृषि वानिकी प्रोत्साहन योजना” का लाभ लें।
-
मनरेगा और वन विभाग की निःशुल्क पौध वितरण योजनाओं का उपयोग करें।
-
कम लागत वाले स्थानीय पौधों का चयन करें।
चुनौती 5: उत्पादों के लिए बाजार की कमी
लकड़ी, गम, चारकोल, फल और पत्तियों के लिए संगठित बाजार हर जगह नहीं मिलता।
समाधान:
-
FPO या किसान उत्पादक संगठन से जुड़ें।
-
कृषि वानिकी आधारित उद्योगों (मुर्गीखाना, मधुमक्खी पालन, मशरूम) के साथ जुड़ाव बढ़ाएँ।
-
उत्पाद को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया, WhatsApp Business और ई-मार्केट प्लेटफॉर्म अपनाएँ।
9.4 नीतिगत और कानूनी चुनौतियाँ
चुनौती 6: कुछ पेड़ों की कटाई पर सरकारी प्रतिबंध
सागौन, नीम, शीशम जैसी पेड़ों की कटाई कुछ राज्यों में अनुमति के बिना संभव नहीं।
समाधान:
-
स्थानीय वन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कटाई अनुमति नियम पढ़ें।
-
ऐसे पेड़ चुनें जिन पर कटाई अनुमति की आवश्यकता न हो।
-
कृषि वानिकी के लिए अनुमोदित प्रजातियों की सूची का पालन करें।
9.5 प्राकृतिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ
चुनौती 7: कीट व रोग का प्रकोप
कुछ पेड़ और फसलें एक-दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं।
समाधान:
-
नीम, करंज जैसे प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करें।
-
फसल चक्र और मिश्रित खेती अपनाएँ।
-
समय-समय पर फसल एवं पेड़ों का निरीक्षण करें।
चुनौती 8: प्राकृतिक आपदाएँ (सूखा, बाढ़, तेज हवाएँ)
समाधान:
-
हवा रोकने वाली पंक्तियाँ (windbreaks) लगाएँ।
-
नालियाँ बनाकर अतिरिक्त पानी बाहर निकालें।
-
सूखा-रोधी प्रजातियाँ (जैसे अरहर, मोरिंगा, बेर) लगाएँ।
9.6 सामाजिक चुनौतियाँ
चुनौती 9: किसानों में जागरूकता की कमी
कई किसान अभी भी कृषि वानिकी के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते।
समाधान:
-
किसानों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ आयोजित करें।
-
KVK, कृषि विश्वविद्यालय और NGO की मदद लें।
-
सफल कृषि वानिकी मॉडलों के प्रदर्शन प्लॉट बनाएँ।
9.7 श्रम एवं समय प्रबंधन की चुनौती
चुनौती 10: पेड़ और फसल दोनों का प्रबंधन कठिन
समाधान:
-
श्रम बचाने वाली तकनीकें अपनाएँ (ड्रिप, मल्चिंग, उन्नत कृषि उपकरण)।
-
परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर कार्य विभाजन करें।
-
पेड़ प्रबंधन का वार्षिक कैलेंडर बनाएं।
भाग 9 का सारांश (Quick Summary)
✔ पेड़–फसल चयन, जल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और बाजार—कृषि वानिकी की मुख्य चुनौतियाँ
✔ सरकारी योजनाएँ, वैज्ञानिक मॉडल, उचित प्रबंधन और प्रशिक्षण—सभी चुनौतियों का समाधान
✔ सही योजना के साथ कृषि वानिकी अधिक लाभदायक और टिकाऊ कृषि पद्धति
भाग 10: कृषि वानिकी में सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ
भाग 10: कृषि वानिकी में सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ (Government Schemes & Policies in Agroforestry)
भारत सरकार एवं राज्य सरकारें कृषि वानिकी (Agroforestry) को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ, सब्सिडी, नीतियाँ और कानून प्रदान करती हैं। इनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण करना, तथा वानिकी आधारित कृषि मॉडल को अपनाने में सहायता देना है।
10.1 राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (National Agroforestry Policy – 2014)
भारत विश्व का पहला देश है जिसने 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति लागू की। इसके उद्देश्य:
मुख्य लक्ष्य
-
खेतों में अधिक पेड़ लगाना (Tree Outside Forest – TOF)
-
किसानों को लकड़ी बेचने की स्वतंत्रता देना
-
कृषि वानिकी के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन
-
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटना
नीति के प्रमुख लाभ
-
पेड़ कटाई के नियम सरल किए गए
-
कई राज्यों में अनुमति (permit) की आवश्यकता खत्म
-
किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध उपलब्ध कराने की व्यवस्था
-
कृषि–वानिकी को राष्ट्रीय स्तर पर कृषि योजनाओं में शामिल किया गया
10.2 हरित भारत मिशन (Green India Mission – GIM)
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शुरू की गई इस योजना का एक महत्वपूर्ण भाग कृषि वानिकी को बढ़ावा देना है।
लाभ:
-
किसानों को निःशुल्क या सब्सिडी पर पौधे
-
किसानों के खेतों में वृक्षारोपण की विशेष योजना
-
प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता
-
जल संरक्षण और मिट्टी सुधार परियोजनाएँ
10.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)
MGNREGA के तहत कृषि वानिकी को विशेष समर्थन मिलता है।
किसानों के लिए लाभ:
-
खेतों में पौधारोपण के लिए मजदूरी सरकार देती है
-
पौधों की सुरक्षा (फेंसिंग) और सिंचाई पर भी सहायता
-
छोटे व सीमांत किसानों को लागत कम करने में मदद
-
वर्षा जल संचयन निर्माण भी इसी योजना से संभव
10.4 राष्ट्रीय कृषक विकास योजना (RKVY – Rashtriya Krishi Vikas Yojana)
इस योजना के तहत कृषि विश्वविद्यालयों और KVK के माध्यम से कृषि वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाता है।
लाभ:
-
पौध उत्पादन नर्सरी स्थापित करने के लिए फंड
-
किसानों के लिए प्रशिक्षण
-
उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की उपलब्धता
-
नई तकनीकों का प्रसार
10.5 एकीकृत बागवानी मिशन (MIDH - Mission for Integrated Development of Horticulture)
फलदार पेड़ों (Horti-Agri मॉडल) को अपनाने वाले किसानों के लिए बेहतरीन योजना।
मुख्य लाभ:
-
आम, अमरूद, बेर, आँवला, नींबू जैसे पौधों पर सब्सिडी
-
ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी
-
बागान विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता
-
पौधों की नर्सरी पर अनुदान
10.6 राज्य सरकारों की विशेष कृषि वानिकी योजनाएँ
(A) उत्तर प्रदेश किसान कृषि वानिकी योजना
-
नीलगिरी, पॉपलर, शीशम, महुआ पर विशेष प्रोत्साहन
-
कटाई अनुमति प्रक्रिया सरल
(B) महाराष्ट्र कृषि वानिकी मिशन
-
खेती के मुताबिक पौध चयन की विशेषज्ञ सहायता
-
मुफ्त पौध वितरण और प्रशिक्षण
(C) मध्य प्रदेश कृषि वानिकी प्रोत्साहन
-
नलकूप, ड्रिप इरिगेशन और पौध संरक्षण पर अनुदान
-
बांबू मिशन (Special Bamboo Mission)
(D) पंजाब और हरियाणा कृषि वानिकी नीति
-
पॉपलर और नीलगिरी के रोपण पर विशेष समर्थन
-
कटाई और परिवहन नियम आसान
नोट: आपके राज्य की स्थानीय नीतियाँ अलग-अलग हो सकती हैं।
10.7 कृषि वानिकी में कटाई और परिवहन कानून
पहले किसानों को पेड़ काटने और बेचने के लिए बहुत कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती थीं।
अब सरकार ने इन नियमों को काफी सरल किया है।
मुख्य प्रजातियाँ — जिन पर अधिकांश राज्यों में अनुमति की आवश्यकता नहीं
-
नीलगिरी (Eucalyptus)
-
पॉपलर (Poplar)
-
बांस (Bamboo – अब घास की श्रेणी में)
-
सुभाभूल (Subabul)
-
नीम (Azadirachta indica) – कई राज्यों में मुक्त
-
सागौन (Teak) – कुछ राज्यों में सरल अनुमति
सरल किए गए नियम:
-
कटाई अनुमति (Tree Felling Permit) ऑनलाइन
-
परिवहन के लिए एक ही दस्तावेज पर्याप्त
-
FPO के माध्यम से सामूहिक बिक्री
10.8 कार्बन क्रेडिट और कृषि वानिकी
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि वानिकी कार्बन क्रेडिट कमाने का बड़ा स्रोत बन रहा है।
किसान को लाभ कैसे मिलता है?
-
पेड़ों द्वारा अवशोषित CO₂ का मूल्य मिलता है
-
FPO या NGO के माध्यम से कार्बन ट्रेडिंग
-
अतिरिक्त आय स्रोत
भारत सरकार भी इस दिशा में नई नीतियाँ तैयार कर रही है।
10.9 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
कृषि वानिकी में ड्रिप सिंचाई और माइक्रो इरिगेशन का महत्वपूर्ण योगदान है।
लाभ:
-
ड्रिप इरिगेशन पर 55–75% तक सब्सिडी
-
मल्चिंग, फर्टिगेशन जैसी तकनीकें अपनाने पर सहायता
10.10 किसान उत्पादक संगठन (FPO) योजना
कृषि वानिकी उत्पादों को बेचने में FPO महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
लाभ:
-
सामूहिक विपणन
-
बेहतर दाम
-
प्रोसेसिंग इकाई लगाने में सहायता
-
सरकार द्वारा 15 लाख तक की आर्थिक मदद
भाग 10 का सारांश (Quick Summary)
✔ भारत कृषि वानिकी नीति अपनाने वाला पहला देश
✔ पौधारोपण, कटाई, विपणन, सिंचाई — हर क्षेत्र में सरकारी सहायता
✔ MGNREGA, MIDH, GIM, PMKSY जैसी योजनाएँ किसानों को कम लागत पर शुरुआत करने में मदद करती हैं
✔ FPO, कार्बन क्रेडिट और बांस मिशन किसानों की आय बढ़ाने में सहायक
भाग 11: कृषि वानिकी में आर्थिक लाभ और लागत विश्लेषण
भाग 11: कृषि वानिकी में आर्थिक लाभ और लागत विश्लेषण (Economic Benefits & Cost Analysis in Agroforestry)
कृषि वानिकी (Agroforestry) एक बहुआयामी खेती पद्धति है, जो किसान को न केवल स्थिर आय देती है बल्कि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। फसल, पेड़, पशुपालन और अन्य उत्पादों से कई स्तरों पर आय उत्पन्न होती है। इस अध्याय में आर्थिक लाभ, लागत संरचना और वास्तविक गणना को विस्तार से समझाया गया है।
11.1 कृषि वानिकी का आर्थिक महत्व
कृषि वानिकी पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक लाभदायक, जोखिम-रहित और सतत आय प्रदान करती है।
मुख्य आर्थिक विशेषताएँ
-
एक ही भूमि से एकाधिक आय स्रोत
-
कम जोखिम और अधिक स्थिरता
-
बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित
-
लंबी अवधि में पेड़ की लकड़ी से बड़ा लाभ
-
इनपुट लागत कम होने से शुद्ध लाभ अधिक
11.2 कृषि वानिकी में आय के प्रमुख स्रोत
(A) फसलों से आय
-
अनाज (गेहूँ, धान)
-
दालें
-
सब्जियाँ
-
तिलहन
(B) वृक्षों से आय
-
लकड़ी
-
इंधन (Fuel wood)
-
गोंद (Gum)
-
बांस
-
औषधीय पत्तियाँ
(C) फलदार पेड़ों से आय
-
आम, अमरूद, नींबू, बेर आदि
(D) पशुपालन से आय (अगर Silvo-Pastoral मॉडल अपनाया हो)
-
दूध, मांस, पशु
-
चारा उत्पादन
(E) अतिरिक्त स्रोत
-
मधुमक्खी पालन (Beekeeping)
-
कार्बन क्रेडिट
-
चारकोल और पलायन उद्योग
-
पत्तों से जैव-खाद
11.3 प्रारंभिक लागत (Initial Investment Cost)
एक सामान्य 1 हेक्टेयर कृषि वानिकी मॉडल के लिए अनुमानित लागत:
| घटक | लागत (₹ में) |
|---|---|
| पौध (200–600 पेड़) | 5,000 – 20,000 |
| गड्ढे की खुदाई व रोपण | 10,000 – 25,000 |
| सिंचाई व्यवस्था (ड्रिप) | 30,000 – 45,000 |
| खाद/खरपतवार प्रबंधन | 5,000 – 15,000 |
| फेंसिंग | 15,000 – 35,000 |
| श्रम लागत | 8,000 – 20,000 |
| कुल प्रारंभिक लागत | 73,000 – 1,60,000 रुपये |
(लागत राज्य, फसल और पेड़ के प्रकार के अनुसार बदल सकती है)
11.4 वार्षिक रखरखाव लागत (Annual Maintenance Cost)
| कार्य | लागत (₹ में/वर्ष) |
|---|---|
| सिंचाई व देखभाल | 5,000 – 10,000 |
| छंटाई/काट-छाँट | 3,000 – 6,000 |
| जैविक खाद | 2,000 – 5,000 |
| श्रम | 5,000 – 10,000 |
| कुल वार्षिक लागत | 15,000 – 30,000 रुपये |
11.5 आर्थिक लाभ (Projected Earnings)
नीचे कुछ आम कृषि वानिकी मॉडलों के संभावित लाभ दिए गए हैं:
(A) Agri-silviculture Model (फसल + पेड़)
उदाहरण: गेहूँ + सागौन (Teak)
आय:
-
फसल आय: ₹50,000 – 80,000 /वर्ष
-
पेड़ आय (8–10 वर्ष बाद): ₹6–10 लाख /हेक्टेअर
शुद्ध लाभ:
कुल लाभ 8 वर्षों में: लगभग ₹10–14 लाख
(B) Horti-Agri Model (फल + फसल)
उदाहरण: आम + दलहन
आय:
-
फसल आय: ₹40,000 – 70,000/वर्ष
-
फल आय (3–5 वर्ष बाद): ₹60,000 – 2,00,000/वर्ष
शुद्ध लाभ:
5वें वर्ष के बाद हर साल ₹1.2 से 2.5 लाख आय
(C) Silvo-Pastoral Model (पेड़ + चरागाह + पशुपालन)
आय:
-
चारा: ₹20,000 – 40,000/वर्ष
-
दूध/पशुपालन: ₹60,000 – 1,50,000/वर्ष
-
लकड़ी आय (10 वर्ष): ₹4–8 लाख
(D) Bamboo-based Agroforestry
आय:
-
बांस की बिक्री (3 से 4 वर्ष बाद): ₹60,000 – 1,50,000/वर्ष
-
अतिरिक्त आय: फर्नीचर, हस्तशिल्प, कागज उद्योग
11.6 लाभ-लागत अनुपात (Benefit–Cost Ratio, BCR)
कृषि वानिकी में BCR सामान्यतः उच्च होता है:
| मॉडल | BCR |
|---|---|
| Agri-Silviculture | 1 : 3.5 |
| Horti-Agri | 1 : 4.2 |
| Bamboo Model | 1 : 5.0 |
| Silvo-Pastoral | 1 : 3.8 |
यानी हर 1 रुपये निवेश पर 3.5 से 5 रुपये तक का लाभ।
11.7 जोखिम कम और लाभ अधिक (Low Risk, High Return)
कृषि वानिकी की सबसे बड़ी विशेषता:
✔ पेड़ लंबी अवधि की एकमुश्त बड़ी आय देते हैं
✔ फसल से नियमित आय बनी रहती है
✔ प्राकृतिक आपदाएँ होने पर भी पूरी आय खत्म नहीं होती
✔ पेड़ प्रीमियम बाजार में हमेशा बिकते हैं
11.8 कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय
किसान कार्बन ट्रेडिंग से अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं:
-
1 हेक्टेयर में 200+ पेड़ → 8–12 टन CO₂/year कैप्चर
-
मूल्य: ₹3000 – 7000 प्रति टन
-
वार्षिक आय: ₹25,000 – 60,000
11.9 5-वर्षीय अनुमानित लाभ विश्लेषण (Model Calculation)
एक औसत किसान, जिसने Horti-Agri Model अपनाया:
| वर्ष | आय (₹) | खर्च (₹) | शुद्ध लाभ (₹) |
|---|---|---|---|
| वर्ष 1 | 60,000 | 90,000 | -30,000 |
| वर्ष 2 | 70,000 | 25,000 | 45,000 |
| वर्ष 3 | 90,000 | 25,000 | 65,000 |
| वर्ष 4 | 1,50,000 | 25,000 | 1,25,000 |
| वर्ष 5 | 2,20,000 | 30,000 | 1,90,000 |
कुल शुद्ध लाभ (5 वर्ष): ₹3,95,000
(इसके बाद हर साल लाभ लगातार बढ़ता है)
11.10 भाग 11 का सारांश (Quick Summary)
✔ कृषि वानिकी कई स्त्रोतों से आय प्रदान करती है
✔ प्रारंभिक लागत थोड़ी अधिक, पर दीर्घकालिक लाभ बहुत ज्यादा
✔ लाभ–लागत अनुपात (BCR) सामान्य खेती से 2–3 गुना अधिक
✔ कार्बन क्रेडिट, फल, लकड़ी और पशुपालन से अतिरिक्त आय
✔ कृषि वानिकी = कम जोखिम + स्थिर आय + बड़ा दीर्घकालिक लाभ
भाग 12: कृषि वानिकी में जोखिम प्रबंधन और संरक्षण उपाय(Risk Management & Protection Measures in Agroforestry)
कृषि वानिकी एक स्थायी, लाभदायक और बहुआयामी खेती प्रणाली है, लेकिन इसके साथ कई संभावित जोखिम भी जुड़े होते हैं — जैसे मौसम की अनिश्चितता, कीट–रोग का प्रकोप, बाजार उतार-चढ़ाव, पशु नुकसान और कानूनी बाधाएँ। इन जोखिमों का सही प्रबंधन आवश्यक है ताकि किसान अपनी आय और उत्पादन को सुरक्षित रख सकें।
यह अध्याय कृषि वानिकी में अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधन तरीकों और संरक्षण उपायों को विस्तृत रूप से समझाता है।
12.1 कृषि वानिकी में प्रमुख जोखिमों के प्रकार
✔ जलवायु संबंधी जोखिम (सूखा, बाढ़, तूफ़ान, ओलावृष्टि)
✔ जैविक जोखिम (कीट, रोग, फफूंद, जंगली जानवरों का हमला)
✔ आर्थिक जोखिम (बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव, लागत बढ़ना)
✔ नीतिगत/कानूनी जोखिम (पेड़ कटाई नियम, अनुमति प्रक्रिया)
✔ प्रबंधन जोखिम (गलत फसल–पेड़ संयोजन, रखरखाव की कमी)
12.2 जलवायु संबंधी जोखिम और उनके समाधान
जोखिम 1: सूखा और पानी की कमी
पेड़ और फसलों दोनों की वृद्धि पर असर पड़ता है।
समाधान:
-
ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो-स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग
-
वर्षा जल संचयन (Farm Pond, Check Dam)
-
ज्यादा सूखा-रोधी प्रजातियाँ जैसे:
-
बेर, मोरिंगा, अर्जुन, करंज, नीम
-
-
मल्चिंग से मिट्टी की नमी संरक्षित करें
जोखिम 2: बाढ़ और जलजमाव
समाधान:
-
खेत में जल निकासी नालियाँ बनाना
-
पानी सहन करने वाली प्रजातियाँ:
-
बाँस, अर्जुन, खैर
-
-
ऊँची मेंड़ या रेज्ड बेड (raised bed) बनाना
जोखिम 3: तेज हवाएँ / तूफ़ान
समाधान:
-
खेत के चारों ओर विंडब्रेक (Windbreak Trees) लगाएँ
-
अच्छे विकल्प:
-
अरुंडी, सरो, शीशम, पॉपलर
-
-
कमजोर और ऊँची प्रजातियों को सहारा (support sticks) दें
12.3 जैविक जोखिम और संरक्षण तकनीकें
जोखिम 4: कीट और रोग का प्रकोप
समाधान:
-
Integrated Pest Management (IPM) अपनाएँ
-
नीम, दशपर्णी अर्क, लस्सी अर्क जैसे जैविक स्प्रे
-
कीट-रोधी पेड़–फसल का संयोजन
-
समय-समय पर नियमित निगरानी (Monitoring)
-
फसल चक्र (Crop Rotation) अपनाएँ
जोखिम 5: जंगली/घरेलू पशुओं का नुकसान
गाय, बकरी, नीलगाय, सूअर आदि पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं।
समाधान:
-
कंटीली तार या सोलर फेंसिंग
-
जीव-जंतु रोधी पौधे जैसे करंज, बबूल, कनेर खेत की मेंड़ों पर लगाएँ
-
बांस या लोहे की सुरक्षा जैकेट पौधों के लिए
12.4 आर्थिक और बाजार संबंधी जोखिम
जोखिम 6: उत्पादन मूल्य में गिरावट
समाधान:
-
फसलों और पेड़ों में विविधता रखें (दोगुनी सुरक्षा)
-
FPO के साथ जुड़कर सामूहिक विपणन
-
फल और लकड़ी प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ें
-
भंडारण (Storage) की व्यवस्था करें
-
ऑनलाइन/डायरेक्ट मार्केटिंग अपनाएँ (WhatsApp, ONDC, ई-मंडी)
जोखिम 7: लागत बढ़ना और लाभ कम होना
समाधान:
-
जैविक खाद से लागत कम करें
-
बेहतर समय पर रोपण करें
-
सरकारी सब्सिडी योजनाओं का उपयोग (PMKSY, MIDH, RKVY)
-
कम लागत वाले स्थानीय पौध चुनें
12.5 प्रबंधन संबंधी जोखिम
जोखिम 8: गलत पेड़–फसल संयोजन
समाधान:
-
गहरी जड़ वाले पेड़ + उथली जड़ वाली फसलें
-
छाया सहनशील फसलें (हल्दी, अदरक, अरबी) पेड़ों के नीचे
-
स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से सलाह लें
जोखिम 9: तकनीकी ज्ञान की कमी
समाधान:
-
नियमित प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ, ऑनलाइन कोर्स
-
KVK, कृषि विश्वविद्यालयों और वन विभाग से सहयोग
-
कृषि वानिकी मॉडल प्लॉट का अवलोकन
12.6 कानूनी जोखिम और समाधान
जोखिम 10: पेड़ कटाई और परिवहन संबंधी कानून
समाधान:
-
कृषि वानिकी नीति 2014 के तहत कई नियम सरल हुए
-
अनुमति-रहित प्रजातियाँ चुनें (पॉपलर, बांस, नीलगिरी)
-
e-Permit प्रणाली का उपयोग
12.7 अन्य संरक्षण उपाय
✔ मिट्टी संरक्षण उपाय
-
कंटूर बंडिंग
-
हेजरो (Hedgerow)
-
कवर क्रॉप
✔ आग से सुरक्षा
-
फायर लाइन बनाना
-
सूखी पत्तियाँ न जलाएं
-
हरित अवरोधक लगाना
✔ तकनीकी संरक्षण
-
ड्रोन से फसल निगरानी
-
मिट्टी परीक्षण
-
मौसम पूर्वानुमान ऐप (IMD, Kisan Suvidha)
भाग 12 का सारांश (Quick Summary)
✔ जोखिम चार तरह के — जलवायु, जैविक, आर्थिक, कानूनी
✔ IPM, ड्रिप, मल्चिंग, फेंसिंग, विंडब्रेक — प्रमुख संरक्षण उपाय
✔ पेड़–फसल विविधता = जोखिम कम + आय स्थिर
✔ तकनीकी ज्ञान + सरकारी नीतियाँ → कृषि वानिकी अधिक सुरक्षित
✔ सही प्रबंधन से अधिकांश जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है
भाग 13: कृषि वानिकी के सफल केस स्टडी (Case Studies)
इस अध्याय में हम भारत और विश्व के कुछ प्रमुख सफल कृषि वानिकी मॉडल्स, किसानों के वास्तविक अनुभव, और अपनाई गई तकनीकों का अध्ययन करेंगे। इसका उद्देश्य पाठकों को प्रेरित करना और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है।
13.1 केस स्टडी 1: महाराष्ट्र – आम + दलहन आधारित कृषि वानिकी मॉडल
किसान: श्री रामकृष्ण जाधव, सोलापुर
क्षेत्र: 5 एकड़
मॉडल: आम + तुर (अरहर) + चारा घास
रणनीति
-
25×25 फीट की दूरी पर आम के पेड़ लगाए
-
खाली जगह में हर वर्ष तुर और मौसमी दालें
-
खेत के किनारों पर नेपियर चारा घास
परिणाम
-
तीसरे वर्ष से आम की कम उपज, सातवें वर्ष से व्यावसायिक उत्पादन
-
हर वर्ष तुर से अच्छी नकद आय
-
पशुओं के लिए चारा की सुनिश्चित उपलब्धता
-
मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी, पानी की बचत
वार्षिक आय
₹2.5–3 लाख (7वें वर्ष के बाद)
13.2 केस स्टडी 2: उत्तर प्रदेश – पॉपलर आधारित एग्रोफोरेस्ट्री मॉडल
किसान: मनोज चौधरी, सहारनपुर
क्षेत्र: 6 एकड़
मॉडल: पॉपलर + आलू + गेहूँ
रणनीति
-
6×6 फीट पर पॉपलर रोपण
-
शुरुआती वर्षों में खेत पूरी तरह खुला, फसलें अच्छी हुईं
-
पॉपलर की तेजी से बढ़त, 6–7 साल में कटाई
परिणाम
-
6 साल में प्रति पेड़ 12–15 हजार रुपये का मूल्य
-
इंटरक्रॉप से हर वर्ष स्थिर आय
-
किसान लकड़ी मंडी से सीधे बेचकर उच्च लाभ कमा पाए
कुल आय (6 वर्ष में)
₹18–22 लाख
13.3 केस स्टडी 3: राजस्थान – खेजड़ी + बाजरा मॉडल (शुष्क क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण)
किसान: मीठालाल विश्नोई, बाड़मेर
क्षेत्र: 15 एकड़
मॉडल: खेजड़ी + बाजरा + चारागाह प्रणाली
रणनीति
-
प्राकृतिक रूप से उगने वाली खेजड़ी को संरक्षित किया
-
खेत में बाजरा और हरी चटनी (फॉडर) की खेती
-
पानी संरक्षण खाल और मेड़बंदी तकनीक
परिणाम
-
खेजड़ी पेड़ों ने मिट्टी को संरक्षित किया
-
सूखे वर्षों में भी 40–50% तक स्थिर उपज
-
पशुपालन + फसल + लकड़ी का बहु-आय स्रोत
वार्षिक आय
₹5–6 लाख (सूखे क्षेत्रों में उत्कृष्ट)
13.4 केस स्टडी 4: केरल – रबर आधारित कृषि वानिकी मॉडल
किसान: थॉमस वरगेज़े, कोट्टायम
क्षेत्र: 4 एकड़
मॉडल: रबर + केले + अदरक + हल्दी
रणनीति
-
रबर के पेड़ों के नीचे छाया-सहिष्णु फसलों का चयन
-
मिट्टी संरक्षण हेतु मल्चिंग
-
जैविक खाद का उपयोग
परिणाम
-
रबर से नियमित आय
-
केला, अदरक, हल्दी से साल में 2–3 बार नकदी प्रवाह
-
मिट्टी की संरचना और नमी में सुधार
वार्षिक संयुक्त आय
₹4–5 लाख
13.5 केस स्टडी 5: मध्यप्रदेश – महुआ + कंद-मूल मॉडल
किसान: लक्ष्मण सिंह, मंडला
क्षेत्र: 12 एकड़
मॉडल: महुआ + शकरकंद + अरबी + कोदो-कुटकी
रणनीति
-
वानिकी और आदिवासी खाद्य फसलों का मिश्रण
-
महुआ को केंद्र में रखते हुए मिश्रित कृषि
-
देसी बीजों का उपयोग
परिणाम
-
महुआ से वार्षिक उच्च मूल्य
-
कंद-मूल फसलों से खाद्य सुरक्षा
-
कृषि वानिकी ने भूमि की उत्पादकता बढ़ाई
वार्षिक कुल आय
₹3–4 लाख
13.6 केस स्टडी 6: अंतरराष्ट्रीय उदाहरण – केन्या का “एग्रोफॉरेस्ट पार्कलैंड सिस्टम”
मॉडल: एकाशिया + मक्का + पशुपालन
रणनीति
-
पेड़ों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण
-
छाया और हवा संरक्षण
-
चराई नियंत्रण और भूमि प्रबंधन
परिणाम
-
20–30% तक फसल सुधार
-
मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि
-
जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन
13.7 इन केस स्टडी से मिलने वाली सीख
-
बहु-आय मॉडल सबसे सफल होते हैं
-
पेड़ + फसल + पशुपालन का संयोजन अधिक लाभदायक है
-
सही पौधों का चयन 70% सफलता सुनिश्चित करता है
-
दीर्घकालीन योजना, जल-संरक्षण और मिट्टी सुधार से आय स्थिर रहती है
-
सरकारी योजनाओं और बाजार से सीधे जुड़ाव से आय कई गुना बढ़ती है
भाग 14: भविष्य में कृषि वानिकी की संभावनाएँ (Future Prospects)
कृषि वानिकी आने वाले दशकों में कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनने जा रही है। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण, और किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता के बीच कृषि वानिकी एक स्थायी और लाभदायक समाधान के रूप में उभर रही है।
14.1 जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में कृषि वानिकी का महत्व
-
कृषि वानिकी कार्बन अवशोषण का सबसे प्रभावी साधन है।
-
पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं।
-
छाया और नमी संरक्षण से जलवायु जोखिम (सूखा, लू, बाढ़) कम होता है।
-
भविष्य में सरकारें कार्बन क्रेडिट जैसी योजनाओं में कृषि वानिकी को प्राथमिकता देंगी।
14.2 किसानों की आय दोगुनी करने में योगदान
-
एक ही भूमि से फसल + फल + लकड़ी + चारा + औषधीय पौधों से बहु-आय
-
बाजार मूल्य अधिक होने से वित्तीय सुरक्षा
-
लकड़ी उद्योग और बागवानी उद्योग की बढ़ती मांग से भविष्य में आय और बढ़ेगी
-
प्रसंस्करण उद्योग (जैसे– नींबू, आम, महुआ, बबूल) से किसानों की भूमिका मज़बूत होगी
14.3 कार्बन क्रेडिट और ग्रीन मार्केट का बढ़ता महत्व
-
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर “कार्बन क्रेडिट मार्केट” तेजी से बढ़ रहा है
-
कृषि वानिकी करने वाले किसानों को पेड़ों द्वारा अवशोषित कार्बन का भुगतान मिल सकता है
-
भविष्य में यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का बड़ा स्रोत बनेगा
14.4 कृषि-वनीकरण आधारित उद्योगों की वृद्धि
आने वाले वर्षों में निम्नलिखित उद्योग तेज़ी से बढ़ने वाले हैं:
-
लकड़ी और प्लाईवुड उद्योग
-
पेपर मिलें
-
हर्बल और आयुर्वेदिक दवा उद्योग
-
फल प्रसंस्करण यूनिट
-
बायोफ्यूल और बायोएनर्जी सेक्टर
इन उद्योगों में रोजगार और बाजार की मांग लगातार बढ़ेगी।
14.5 जल संरक्षण और भूमि पुनर्स्थापन में भूमिका
-
पेड़ों की जड़ें मिट्टी कटाव रोकती हैं और जलधारण क्षमता बढ़ाती हैं
-
सूखे इलाकों में कृषि वानिकी जल स्तर बढ़ाने में सहायक
-
खराब, बंजर या क्षतिग्रस्त भूमि को पुनर्जीवित करने में कृषि वानिकी सर्वोत्तम तरीका
-
भविष्य में सरकारें “लैंड रेस्टोरेशन मिशन” में इसे प्राथमिकता देंगी
14.6 जलवायु-स्मार्ट कृषि का आधार
कृषि वानिकी आने वाले समय में "Climate Smart Agriculture" की मुख्य तकनीक मानी जाएगी।
यह प्रणालियाँ किसानों को तैयार करती हैं:
-
जलवायु जोखिम का सामना करने के लिए
-
अधिक उत्पादन के लिए
-
पर्यावरण-सुरक्षित खेती के लिए
-
बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए
14.7 युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए अवसर
अगले 10–20 वर्षों में कृषि वानिकी क्षेत्र में स्टार्टअप्स की बड़ी संभावनाएँ होंगी:
-
नर्सरी और पौध उत्पादन
-
टिश्यू कल्चर आधारित पौधे
-
फल प्रसंस्करण यूनिट
-
लकड़ी आधारित माइक्रो-उद्योग
-
कार्बन क्रेडिट कंसल्टेशन
-
सस्टेनेबल खेती पर ट्रेनिंग और एडवाइजरी
यह क्षेत्र ग्रामीण उद्यमिता को नई दिशा देगा।
14.8 तकनीकी प्रगति और डिजिटल कृषि वानिकी
भविष्य में निम्न तकनीकें कृषि वानिकी को और अधिक प्रभावशाली बनाएंगी:
-
ड्रोन आधारित पौधारोपण
-
मिट्टी और जल की रियल-टाइम निगरानी
-
मोबाइल ऐप आधारित बाजार सूचना
-
प्रिसिजन एग्रोफॉरेस्ट्री
-
GIS और रिमोट सेंसिंग से भूमि विश्लेषण
-
AI आधारित फसल और पेड़ चयन मॉडल
14.9 वैश्विक स्तर पर बढ़ता महत्व
-
संयुक्त राष्ट्र (UN), FAO, और IPCC कृषि वानिकी को भविष्य का समाधान मानते हैं
-
दुनिया भर में किसान—ब्राजील, केन्या, चीन, यूरोप—तेजी से अपनाने लगे हैं
-
भारत अगले वर्षों में Agroforestry Capital बनने की क्षमता रखता है
14.10 भविष्य की चुनौतियाँ (लेकिन हल मौजूद हैं)
-
गुणवत्तापूर्ण पौधों की कमी
-
किसानों में जागरूकता की कमी
-
बाजार जुड़ाव में समस्या
-
लंबी अवधि के निवेश का डर
समाधान
-
सरकारी सहायता और CSR फंडिंग
-
निजी नर्सरी व स्टार्टअप्स
-
फसल-लकड़ी खरीद गारंटी मॉडल
-
किसानों का समूह-आधारित खेती मॉडल
14.11 निष्कर्ष: कृषि वानिकी का भविष्य उज्ज्वल है
कृषि वानिकी न केवल पर्यावरण संरक्षण करती है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी स्थिर और मजबूत बनाती है।
भविष्य में यह स्मार्ट, टिकाऊ और लाभकारी कृषि का मुख्य स्तंभ बनने वाली है।
भाग 15: कृषि वानिकी में प्रशिक्षण और संसाधन
कृषि वानिकी को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए किसानों, छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को उचित प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और विश्वसनीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हम उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थान, ऑनलाइन संसाधन, सरकारी सहायता, पुस्तकों और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के बारे में विस्तार से जानेंगे।
15.1 किसानों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम
भारत में कृषि वानिकी से संबंधित कई सरकारी और निजी संस्थान नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
मुख्य प्रशिक्षण विषय
-
पेड़–फसल संयोजन (Tree–Crop Combination)
-
पौधरोपण और दूरी प्रबंधन
-
माइक्रो इरिगेशन और जल संरक्षण
-
नर्सरी प्रबंधन
-
मिट्टी सुधार और जैविक खाद
-
कार्बन क्रेडिट और लकड़ी विपणन
-
जोखिम प्रबंधन और कीट-रोग नियंत्रण
लाभ
-
व्यवहारिक ज्ञान
-
कम लागत में अपनाने योग्य तकनीक
-
सरकारी योजनाओं की जानकारी
-
किसान–विशेषज्ञ नेटवर्किंग
15.2 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान (भारत में)
1. कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)
-
भारत के हर जिले में स्थित
-
किसानों के लिए 1–3 दिन के फ्री/कम शुल्क के प्रशिक्षण
-
कृषि वानिकी, नर्सरी, वर्मी-कंपोस्ट, फसल प्रबंधन आदि
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थान
-
ICAR-CAFRI (Jhansi) – Agroforestry का राष्ट्रीय केंद्र
-
पौध चयन, मॉडल डिज़ाइन, कार्बन sequestration, रिसर्च
-
लंबे एवं उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
-
किसान क्लब और समूह आधारित प्रशिक्षण
-
वानिकी आधारित FPO बनाने के लिए विशेष कार्यशालाएँ
-
वित्तीय सहायता और स्किल डेवलपमेंट
4. वन विभाग (State Forest Department)
-
पौधरोपण, जल संरक्षण, भूमि उपयोग, वन-पर्यटन से जुड़े कार्यक्रम
-
सस्ती दरों पर पौध उपलब्ध कराना
5. कृषि विश्वविद्यालय
जैसे–
-
GBPUAT (Pantnagar)
-
TNAU (Coimbatore)
-
Dr. PDKV (Akola)
-
पंजाब एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी
-
ये सभी नियमित कृषि वानिकी प्रशिक्षण और डिप्लोमा प्रदान करते हैं।
15.3 ऑनलाइन प्रशिक्षण और ई-लर्निंग संसाधन
1. e-Krishi Manch (ICAR)
-
फ्री कोर्स
-
Agroforestry basics, tree management, soil conservation
2. कृषि मंत्रालय के ऑनलाइन मॉड्यूल
-
PMKSY, RKVY और NMSA से जुड़े प्रशिक्षण
-
वीडियो ट्यूटोरियल और ई-बुक्स
3. YouTube कृषि चैनल
-
कृषि वानिकी पर डेमो
-
नर्सरी प्रबंधन
-
सफलता की कहानियाँ
4. Coursera, edX और FAO Online Courses
-
Sustainable land management
-
Climate-smart agriculture
-
Forest management
5. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म (NREGA, NREGAsoft)
-
भूमि संरक्षण तकनीकों की जानकारी
15.4 फील्ड विज़िट और ऑन-ग्राउंड अध्ययन
कई किसान और छात्र वास्तविक फील्ड विज़िट में जाकर तकनीक सीखते हैं।
उपलब्ध विकल्प
-
ICAR-CAFRI के डेमो प्लॉट
-
वानिकी विभाग के मॉडल फार्म
-
निजी नर्सरी और एग्रोफॉरेस्टिंग फार्म
-
सफल किसानों के खेतों की विज़िट (Farm School Program)
लाभ
-
प्रैक्टिकल ज्ञान
-
तकनीकों को लाइव देखना
-
बिजनेस मॉडल समझना
15.5 प्रशिक्षण में उपयोग होने वाली सामग्री और उपकरण
-
पौधरोपण उपकरण — खुरपी, फावड़ा, मीटर स्केल
-
GIS/Drone आधारित भूमि विश्लेषण सॉफ्टवेयर
-
पोर्टेबल मिट्टी और पानी परीक्षण किट
-
जैविक खाद और मल्चिंग सामग्री
-
पौध पहचान (Tree Identification) चार्ट
-
प्रशिक्षण पुस्तिकाएँ और नोट्स
15.6 भारत सरकार के संसाधन और मार्गदर्शिका
सरकार समय-समय पर कृषि वानिकी से संबंधित गाइड और पुस्तिकाएँ प्रकाशित करती है।
मुख्य प्रकाशन
-
“National Agroforestry Policy – 2014”
-
“NMSA Guidelines”
-
“Tree Outside Forest (TOF) Report”
-
“Agroforestry Best Practices Manual”
इन सभी दस्तावेजों से मॉडल चयन, क्षेत्रीय पौधों और नीतियों की समझ बढ़ती है।
15.7 शोध पत्र, पुस्तकें और अन्य संदर्भ सामग्री
1. कृषि वानिकी पर लोकप्रिय पुस्तकें
-
Agroforestry: Principles and Practices
-
Sustainable Farm Forestry Systems
-
Handbook of Agroforestry
-
Indian Agroforestry Models – ICAR Publication
2. शोध पत्र और जर्नल
-
Indian Journal of Agroforestry
-
Agroforestry Systems (Springer)
-
Journal of Forestry Research
15.8 स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण
कृषि वानिकी आधारित स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं।
मुख्य क्षेत्रों में अवसर
-
नर्सरी व्यवसाय
-
बांस/पॉपलर/नीम आधारित MSME
-
फल प्रसंस्करण यूनिट
-
कार्बन क्रेडिट कंसल्टिंग
-
ड्रोन-आधारित फार्म सर्वे
सहायक संस्थान
-
MSME Development Institutes
-
NABARD Incubation Centers
-
Krishi Vigyan Kendras
-
AIC & RKVY-RAFTAAR incubation programs
15.9 निष्कर्ष: प्रशिक्षण और संसाधन सफलता की कुंजी
कृषि वानिकी को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए
-
सही प्रशिक्षण
-
विश्वसनीय संस्थान
-
फील्ड अनुभव
-
और सतत सीखने की मानसिकता
बहुत महत्वपूर्ण है।
सही दिशा और मार्गदर्शन मिलने पर किसान, छात्र और उद्यमी कृषि वानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि वानिकी (Agroforestry) आज के समय में टिकाऊ, लाभदायक और भविष्य-सुरक्षित कृषि पद्धति के रूप में उभर रही है। बदलती जलवायु, घटती भूमि क्षमता, मिट्टी का क्षरण और बढ़ती आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में कृषि वानिकी किसानों के लिए एक मजबूत और स्थायी विकल्प प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में प्रस्तुत सभी अध्यायों का उद्देश्य किसानों, शोधकर्ताओं, छात्रों और नीति-निर्माताओं को कृषि वानिकी के वैज्ञानिक, व्यावहारिक और आर्थिक पहलुओं की संपूर्ण समझ प्रदान करना है।
16.1 समग्र दृष्टिकोण—पेड़, फसल और पशुपालन का संतुलन
कृषि वानिकी आधुनिक कृषि के लिए आवश्यक "एकीकृत प्रणाली" का प्रतिनिधित्व करती है।
पेड़ + फसल + पशुपालन का संयोजन:
-
भूमि की उत्पादकता बढ़ाता है
-
आय के विविध स्रोत उपलब्ध कराता है
-
जोखिम को कम करता है
-
पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करता है
यह बहु-विषयक मॉडल कृषि को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाता है।
16.2 पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का समाधान
कृषि वानिकी की सबसे बड़ी ताकत इसकी पर्यावरणीय भूमिका है।
यह प्रणाली—
-
कार्बन अवशोषण
-
मिट्टी संरक्षण
-
जल संरक्षण
-
जैव विविधता वृद्धि
-
प्रदूषण नियंत्रण
में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
भविष्य में यह जलवायु-स्मार्ट कृषि की अनिवार्य तकनीक मानी जाएगी।
16.3 किसानों की आय में स्थायी वृद्धि
कृषि वानिकी का बहु-आय मॉडल किसानों को—
-
नियमित लाभ
-
जोखिम रहित आय
-
उच्च मूल्य वाली लकड़ी और फल
-
बाजार से अधिक जुड़ाव
जैसे फायदे प्रदान करता है।
दीर्घकाल में यह मॉडल किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाकर स्थिर आय सुनिश्चित करता है।
16.4 कृषि वानिकी अपनाने की चुनौतियाँ—लेकिन समाधान उपलब्ध
कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं जैसे—
-
लंबी अवधि का निवेश
-
बाजार की अनिश्चितता
-
गुणवत्तापूर्ण पौधों की कमी
-
तकनीकी जानकारी का अभाव
लेकिन पुस्तक में दिए गए समाधान—
-
सरकारी योजनाएँ
-
प्रशिक्षण कार्यक्रम
-
समुदाय आधारित मॉडल
-
अनुसंधान संस्थानों का सहयोग
इन चुनौतियों को प्रभावी तरीके से दूर कर सकते हैं।
16.5 भविष्य की संभावनाएँ अत्यंत उज्ज्वल
अगले 10–20 वर्षों में कृषि वानिकी—
-
कार्बन क्रेडिट मार्केट
-
लकड़ी उद्योग
-
औषधीय पौध उद्योग
-
फल प्रसंस्करण सेक्टर
-
ग्रामीण उद्यमिता
-
डिजिटल कृषि
में नई संभावनाएँ पैदा करेगी।
इसके कारण किसानों, उद्यमियों और निवेशकों के लिए यह क्षेत्र अत्यधिक आकर्षक बन रहा है।
16.6 ज्ञान, प्रशिक्षण और तकनीक—सफलता की कुंजी
कृषि वानिकी को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए तीन तत्व महत्वपूर्ण हैं:
-
सही ज्ञान
-
निरंतर प्रशिक्षण
-
तकनीक का उपयोग
इस पुस्तक में दिए गए सभी चरण, मॉडल, पौध चयन, सरकारी योजनाएँ और केस स्टडी इन्हीं तीन पहलुओं को मजबूत बनाते हैं।
16.7 अंतिम संदेश
कृषि वानिकी केवल खेती की पद्धति नहीं, बल्कि एक जीवनशैली और विचारधारा है—
जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है
और धरती को पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित करती है।
यह पुस्तक आपकी कृषि यात्रा में मार्गदर्शक बने,
आप कृषि वानिकी को अपनाकर समृद्धि की ओर अग्रसर हों—
इसी शुभकामना के साथ निष्कर्ष अध्याय समाप्त होता है।
Terminology (शब्दावली / Glossary)
Terminology (शब्दावली / Glossary)
कृषि वानिकी (Agroforestry) से जुड़ी सामान्य तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली यहाँ सरल भाषा में समझाई गई है। यह Glossary छात्रों, किसानों, शोधकर्ताओं और पाठकों के लिए एक उपयोगी संदर्भ सूची के रूप में तैयार की गई है।
अ
1. कृषि वानिकी (Agroforestry)
पेड़, फसल और पशुपालन को एक साथ प्रबंधन करने वाली टिकाऊ कृषि प्रणाली।
2. अग्रो-इकोसिस्टम (Agro-Ecosystem)
कृषि और प्राकृतिक पर्यावरण का संयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र।
3. अनुशंसित दूरी (Plant Spacing)
पौधों के बीच दी जाने वाली दूरी ताकि सही वृद्धि और उत्पादन हो सके।
आ
4. इंटरक्रॉपिंग (Intercropping)
एक ही खेत में दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की पद्धति।
5. आय-ऊर्जा मॉडल (Income–Energy Model)
कृषि प्रणाली जिसमें आय और ऊर्जा संतुलन का आकलन किया जाता है।
इ
6. इकोलॉजिकल बैलेंस (Ecological Balance)
पर्यावरण में प्रजातियों और संसाधनों का संतुलन।
7. इरिगेशन (Irrigation)
फसलों और पेड़ों को कृत्रिम तरीकों से पानी उपलब्ध कराना।
ई
8. ईको-फ्रेंडली प्रैक्टिसेज़ (Eco-friendly Practices)
ऐसी कृषि पद्धतियाँ जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचातीं।
उ
9. उपज (Yield)
किसी फसल या पेड़ से प्राप्त उत्पादन की मात्रा।
10. उत्तम भूमि उपयोग (Optimal Land Use)
भूमि का अधिकतम और उपयुक्त उपयोग करने का सिद्धांत।
ए
11. एग्रोफॉरेस्ट मॉडल (Agroforestry Model)
पेड़ + फसल/पशु आधारित विशिष्ट कृषि वानिकी प्रणाली।
क
12. कार्बन अवशोषण (Carbon Sequestration)
पेड़ों द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना।
13. कटाव (Soil Erosion)
पानी, हवा या अन्य कारणों से मिट्टी का बह जाना।
14. क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर (Climate Smart Agriculture)
जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकसित कृषि तकनीकें।
ख
15. खनिज पोषक तत्व (Mineral Nutrients)
मिट्टी में मौजूद आवश्यक पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ग
16. ग्रीन कवर (Green Cover)
भूमि पर फैली हरियाली—पेड़, पौधे, घास आदि।
च
17. चराई प्रबंधन (Grazing Management)
पशुओं द्वारा चराई को नियंत्रित और व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करना।
ज
18. जैव विविधता (Biodiversity)
किसी क्षेत्र में उपस्थित वैविध्यपूर्ण जीव-जंतुओं और पौधों की कुल संख्या।
19. जैविक खाद (Organic Manure)
प्राकृतिक स्रोतों से तैयार खाद जैसे गोबर खाद, कम्पोस्ट आदि।
ट
20. ट्री डेंसिटी (Tree Density)
एक निश्चित खेत क्षेत्र में मौजूद पेड़ों की संख्या।
द
21. द्रव्य उत्पादन (Biomass Production)
पौधों द्वारा उत्पन्न कुल जैव द्रव्य (जैविक पदार्थ)।
प
22. पौध चयन (Species Selection)
किसी क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और खेती की जरूरतों के आधार पर सर्वोत्तम पेड़/पौधों का चयन।
23. पॉपलर/यूकेलिप्टस (Poplar/Eucalyptus)
कृषि वानिकी में उपयोग होने वाली तेजी से बढ़ने वाली लकड़ी प्रजातियाँ।
फ
24. फसल चक्र (Crop Rotation)
एक ही जमीन पर अलग-अलग मौसम में अलग फसलें उगाने की प्रक्रिया।
ब
25. बायोड्रेनेज (Biodrainage)
पेड़ों द्वारा अतिरिक्त पानी को अवशोषित करके जलभराव को कम करने की प्रक्रिया।
म
26. मल्चिंग (Mulching)
मिट्टी की नमी और तापमान बनाए रखने के लिए सतह पर जैविक/अजैविक सामग्री बिछाना।
27.模型 पहचान (Model Identification)
किस इलाके के लिए कौन सा एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल उपयुक्त होगा, इसका चयन।
य
28. Yield Gap (उपज अंतर)
संभावित उपज और वास्तविक उपज के बीच का अंतर।
र
29. रूट ज़ोन मैनेजमेंट (Root Zone Management)
जड़ों के क्षेत्र का पोषण प्रबंधन।
व
30. वनस्पति कवर (Vegetative Cover)
भूमि पर फैली सभी प्रकार की हरी वनस्पति।
31. वनीकरण (Afforestation)
खाली या बंजर भूमि पर पेड़ लगाना।
स
32. सिंचाई दक्षता (Irrigation Efficiency)
कम पानी में अधिक सिंचाई प्रभाव प्राप्त करना।
33. Sustainable Farming (टिकाऊ खेती)
ऐसी खेती जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों को संतुलित रखे।
ह
34. हार्वेस्टिंग (Harvesting)
फसल या लकड़ी की कटाई की प्रक्रिया।
English–Hindi Quick Reference
| English Term | Hindi Meaning |
|---|---|
| Agroforestry | कृषि वानिकी |
| Intercropping | अंतरफसल प्रणाली |
| Mulching | मल्चिंग |
| Carbon Sequestration | कार्बन अवशोषण |
| Biomass | जैव द्रव्य |
| Sustainable | टिकाऊ |
| Irrigation | सिंचाई |
| Nursery | पौधशाला |
| Ecosystem | पारिस्थितिकी तंत्र |
👉 Knowledge | Motivation | Skills | Growth
👉Join Our Group: Click
🚀 आज ही जुड़ें और हर दिन सीखें कुछ नया!
AgriGrow Solution
🙏 धन्यवाद! अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे ब्लॉग को फॉलो करें।
🔗 हमसे जुड़े रहें: Facebook | Instagram | Twitter | Telegram | YouTube
💼 हमारी सेवाओं के बारे में जानें: Agriculture | Stock Market | Gyaan Sutra
⚠️ Disclaimer: इस ब्लॉग में दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और सामान्य जानकारी के लिए है। इसमें निवेश, स्वास्थ्य या कानूनी सलाह शामिल नहीं है। किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
© 2025 Mahesh Pawar : सभी अधिकार सुरक्षित। इस ब्लॉग की सामग्री की अनुमति के बिना पुनःप्रकाशन, कॉपी या वितरण निषिद्ध है।

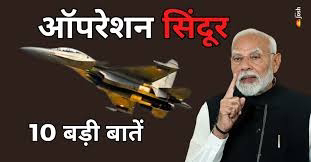


टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thanks for Comment....